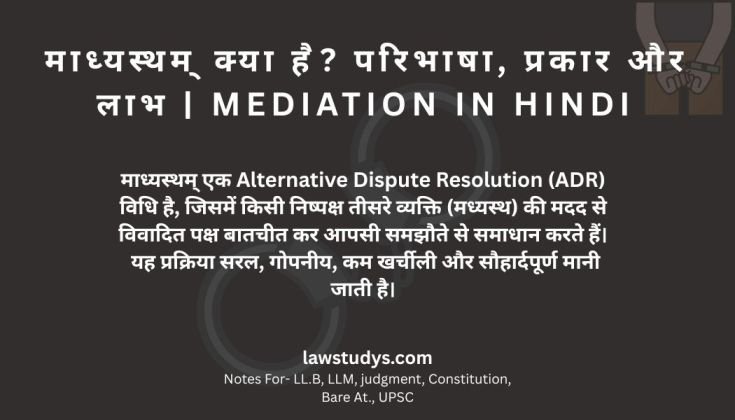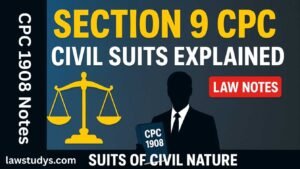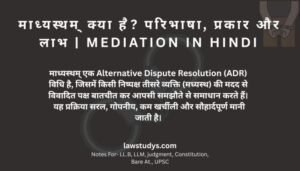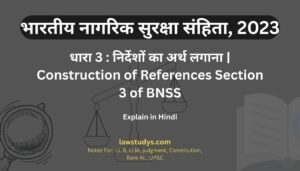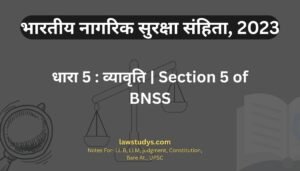‘माध्यस्थम्’ यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रक्रिया है जो विवादों के निपटारों का एक सुलभ एवं सरलतम मंच है। माध्यस्थ के माध्यम से विवादों के निपटारे की यह प्रक्रिया बहुत पुरानी है।
प्राचीनकाल में जब गाँवों, मोहल्लों में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता था तब उस विवाद को समाज के मौजिज व्यक्ति जिन्हें पंच भी कहा जाता था के माध्यम से समाधान किया जाता था। ऐसे पंच गाँव के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे जिन पर पूरा भरोसा एवं विश्वास किया जाता था तथा उनका निर्णय सभी पर आबद्धकर होता था।
वर्तमान में इसी प्रथा को हमने विधि का स्वरूप प्रदान किया और यह ‘माध्यस्थम्’ (Arbitration) के नाम से जानी जाने लगी तथा जिनेवा अभिसमय, 1927 एवं न्यूयार्क अभिसमय, 1958 के अन्तर्गत इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप भी प्रदान किया गया।
माध्यस्थम् क्या है ?
माध्यस्थम् से तात्पर्य, दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा अपने विवादों को निपटाने के लिए तीसरा तटस्थ व्यक्ति जो माध्यस्थ (Arbitrator) होता है को निर्णय के लिए सुपुर्द या सन्दर्भित करने से है जो विवादों का निर्णय न्यायिक तौर पर करता है।
यह भी जाने – राज्य क्या है? परिभाषा, उत्पत्ति एंव राज्य की उत्पत्ति के सिद्वांत
आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि, जब दो या दो से अधिक पक्षकार अपने विवादों को अन्य व्यक्ति की मध्यस्थता से निर्णीत कराने का करार करते है और जिसमें न्यायिक अधिनिर्णय की समस्त औपचारिकताओं का पालन किया जाता है, उसे माध्यस्थम् (Arbitration) कहा जाता है।
माध्यस्थम् में किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति (मध्यस्थ) की सहायता से विवादित पक्षकार आपसी बातचीत और समझौते के द्वारा विवाद का निपटारा करते हैं। यह प्रक्रिया न्यायालय की लंबी कार्यवाही से सरल, तेज़ और कम खर्चे की होती है।
जॉन बी. साउण्डर्स के अनुसार “माध्यस्थम्, दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य विवाद या मतभेद को, दोनों पक्षकारों को न्यायिक रूप पर सुनने के पश्चात, निर्णय के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया गया सन्दर्भ है जो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय नहीं है।”
इस परिभाषा के अनुसार पक्षकार अपने मध्य हुए विवाद को निपटाने के किसी अन्य स्वतंत्र व्यक्ति को नियुक्त करते है, और उसके सामने अपने मामले को रखते है, जो तिसरा व्यक्ति दोनों पक्षों के बात को सुनने के बाद अपना निर्णय देता है, यह निर्णय दोनों पक्षों पर प्रभावी होता है|
यह भी जाने – अनुशासन समिति किसे कहते है? इसका गठन, शक्तियां एंव अधिवक्ता को प्राप्त उपचार
माध्यस्थम् की परिभाषा
कॉलिन्स बनाम कॉलिन्स (28 एल. जे.सी एच, 186) के मामले में माध्यस्थम् की परिभाषा इस तरह दी गई है कि-
“माध्यस्थम्, पक्षकारों के मध्य विशिष्ट विषय-वस्तु पर विवाद या मतभेद का एक या एक से अधिक व्यक्तियों को, अधिनिर्णायक (Umpire) या अधिनिर्णायक के बिना, निर्णय हेतु किया गया सन्दर्भ है।”
माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2(1) (क) के अनुसार – “माध्यस्थम् से कोई माध्यस्थम् अभिप्रेत है जो चाहे स्थायी माध्यस्थम् संस्था द्वारा किया गया हो या नहीं।”
माध्यस्थम् की यह परिभाषा अपूर्ण, संक्षिप्त एवं अस्पष्ट है। वस्तुतः यह माध्यस्थम् शब्द को परिभाषित ही नहीं करती है। माध्यस्थम् की पूर्व में दी गई परिभाषायें ही उपयुक्त है जिनके अनुसार –
(i) माध्यस्थम् दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विवादों का सन्दर्भ (reference) है जो निपटान हेतु किया जाता है;
(ii) ऐसे व्यक्ति को ‘माध्यस्थ’ (Arbitrator) कहा जाता है। जिसे विवाद निपटारे हेतु सन्दर्भित किया जाता है;
(iii) माध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा करार के माध्यम से की जाती है;
(iv) वह सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय नहीं होता है;
(v) वह न्यायालय में संस्थित किया गया वाद भी नहीं है; तथा
(vi) माध्यस्थ द्वारा विवादों का निपटारा दोनों पक्षकारों को न्यायिक तौर पर सुनने के पश्चात् किया जाता है।
यह भी जाने – प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या हैं? इसका महत्व एंव दर्ज कराने की प्रक्रिया | FIR
माध्यस्थम् के प्रकार
माध्यस्थम् तीन प्रकार के होते हैं, जिनका विस्तार से वर्णन किया गया है –
(1) व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम
(2) सांविधिक अर्थात् कानूनी माध्यस्थम
(3) अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम
(1) व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम् (Personal or Domestic Arbitration) :
माध्यस्थम् का यह सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। इसमें दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा अपने विवाद या मतभेद को निर्णय हेतु माध्यस्थम् अधिकरण (Arbitral Tribunal) के सामने रखा जाता है।
माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 में व्यक्तिगत या घरेलू माध्यस्थम् की परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम की परिभाषा दी गई है, जिसके आधार पर व्यक्तिगत या घरेलू माध्यस्थम् को परिभाषित किया जा सकता है।
इसके अनुसार, ऐसा माध्यस्थम जो अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् नहीं है, वह घरेलू माध्यस्थम (Domestic Arbitration) होता है।
घरेलू माध्यस्थम में दोनों पक्षकार भारतीय नागरिक होते हैं, जिसमे विधिक व्यक्ति (Legal person) जैसे कम्पनी, निगम आदि भी हो सकते हैं।
‘कोल इंडिया लिमिटेड बनाम कनाड़ियन कॉमर्शियल कॉरपोरेशन’ (ए.आई.आर. 2012 कलकत्ता 92) के मामले में यह कहा गया है कि- विदेश में दिया गया पंचाट यद्यपि धारा 44 के अन्तर्गत विदेशी पंचाट हो सकता है तथापि वह घरेलू पंचाट भी कहला सकता है यदि वह ऐसे करार के अन्तर्गत दिया गया हो जो करार भारतीय विधि के अधीन किया गया हो।
घरेलू या व्यक्तिगत माध्यस्थमों का सृजन पक्षकारों के करार द्वारा होता है जो करार भारतीय विधि तथा लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिये।
(2) सांविधिक माध्यस्थम् (Statutory Arbitration) :
सामान्यतः माध्यस्थम् की प्रक्रिया का निर्धारण पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से किया जाता है। लेकिन जहाँ ऐसी प्रक्रिया निर्धारित होती है, वहाँ उसी के अनुरूप माध्यस्थम् कार्यवाहियों का संचालन किया जाएगा।
लेकिन कभी-कभी किसी अधिनियम की परिधि में आने वाले विवादों को माध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए उस अधिनियम में प्रक्रिया का उल्लेख भी कर दिया जाता है और उसी प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाहियों का संचालन करना होता है, जैसे :
– माध्यस्थों की नियुक्ति,
– माध्यस्थम् का स्थान,
– पंचाट देने की समयावधि,
– पंचाट का प्रवर्तन,
– माध्यस्थम् कार्यवाहियों पर लागू होने वाली प्रक्रिया,
– माध्यस्थ का शुल्क आदि। ऐसे माध्यस्थम को सांविधिक माध्यस्थम् (Statutory Arbitration) कहा जाता है।
सांविधिक माध्यस्थमों में पक्षकारों की सहमति का कोई स्थान नहीं होता है, पक्षकार सांविधिक उपबन्धों का अनुसरण करने के लिए आबद्ध होते हैं।
सामान्यतया सहकारी समितियाँ अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, विद्युत आपूर्ति अधिनियम आदि में सांविधिक माध्यस्थमों की व्यवस्था होती है।
(3) अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् (International Arbitration)
अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम का सृजन बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की देन है। संचार माध्यमों में अभिवृद्धि तथा राष्ट्रीय व्यापार नीति में उदारीकरण के समावेश से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य में आशातीत वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-वाणिज्य में विवादों एवं मतभेदों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है।
इसी कारण माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 में ऐसे विवादों के निपटारे तथा विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन के बारे में प्रावधान किया गया है। अधिनियम, में ऐसे माध्यस्थमों को ‘अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्’ (International Commercial Arbitration) का कहा है।
अधिनियम की धारा 2(1)(च) के अनुसार- “अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से ऐसे विवादों से सम्बन्धित कोई माध्यस्थम अभिप्रेत है जो ऐसे विधिक सम्बन्धों से उद्भूत हो जो भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन वाणिज्यिक समझे गये हो, चाहे ऐसे विधिक सम्बन्ध संविदात्मक हो या नहीं तथा माध्यस्थम के पक्षकारों में से कम से कम एक पक्षकार निम्न व्यक्तियों में से कोई एक हो-
(i) ऐसा कोई व्याक्त, जो भारत से भिन्न किसी देश का नागरिक है या उसका (भारत से भिन्न किसी देश का) आभ्यासिक निवासी है; या
(ii) ऐसा कोई निगमित निकाय, जो भारत से भिन्न किसी देश में निगमित है; या
(iii) ऐसी कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, जिसका केन्द्रीय प्रबन्ध और नियन्त्रण भारत से भिन्न किसी देश में किया जाता है; या
(iv) विदेशी सरकार
माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 में माध्यस्थम एवं अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है।
माध्यस्थम् के लाभ
माध्यस्थम के अनेक लाभ हैं जिनमें से निम्नांकित मुख्य लाभ है-
(1) सरल एवं द्रुतगामी प्रक्रिया :
माध्यस्थम की प्रक्रिया अत्यन्त सरल एवं द्रुतगामी है क्योंकि इसमें न्यायालय जैसी जटिल प्रक्रिया नहीं है। माध्यस्थम् की कार्यवाहियों पर सिविल प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
अधिवक्ता अथवा विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति की आवश्यकता भी नहीं होती है। कुल मिलाकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों (Principles of Natural Justice) का अनुसरण करना होता है।
(2) खर्चीली एवं विलम्बकारी नहीं होना :
माध्यस्थम की प्रक्रिया न तो व्ययसाध्य है और न ही विलम्बकारी। न्यायालयों में कार्य की अधिकता के कारण मुकदमों के निपटारे में काफी समय लग जाता है तथा व्यय भी अधिक होता है, जबकि माध्यस्थ के समक्ष एक ही विवाद होने से उसका शीघ्र एवं कम व्यय में निपटारा हो जाता है।
माध्यस्थम में सामान्यतः माध्यस्थ को चार माह में और अधिनिर्णायक (Umpire) को दो माह में पंचाट (Award) देना होता है।
(3) पक्षकारों द्वारा माध्यस्थों की नियुक्ति :
माध्यस्थम में माध्यस्थों की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा की जाती है। माध्यस्थ पक्षकारों के विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, अतः माध्यस्थ द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, वह उन्हें सहर्ष स्वीकार होता है तथा पक्षपात की आशंका भी नहीं रहती है, जबकि न्यायालयों के न्यायाधीश सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी सेवक होते हैं जिनके निर्णय पक्षकारों की इच्छा के विपरीत भी हो सकते हैं।
(4) विशेषज्ञ की सेवायें :
माध्यस्थ की नियुक्ति चूंकि पक्षकारों द्वारा की जाती है, अतः वे विवाद की विषयवस्तु के अनुरूप विशेषज्ञ को माध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इससे बेहतर न्याय की सम्भावनायें प्रबल हो जाती हैं, जबकि न्यायालय में न्यायाधीशों का किसी विषय-वस्तु विशेष का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। न्यायालय में विशेषज्ञ मात्र एक साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है जो पर्याप्त नहीं है।
(5) व्यक्तिशः निरीक्षण :
माध्यस्थम का एक लाभ यह भी है कि माध्यस्थ द्वारा स्वयं विवादित स्थल या विषय-वस्तु का निरीक्षण किया जा सकता है जिससे सही निष्कर्ष पर पहुँचने में काफी मदद मिलती है, जबकि न्यायालयों में यह कार्य सामान्यतः स्वयं न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जाकर कमिश्नर द्वारा किया जाता है जो उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होता।
(6) प्राधिकार का प्रतिसंहरण :
माध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि कोई माध्यस्थ भ्रष्ट आचरण या कदाचार (Misconduct) का दोषी है तो पक्षकार द्वारा उसके प्राधिकार का प्रतिसंहरण किया जा सकता है, जबकि न्यायाधीश के प्राधिकार का इस प्रकार प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता।
(7) गोपनीयता :
माध्यस्थम कार्यवाहियाँ सर्वथा गोपनीय होती है। माध्यस्थ भी ऐसी कार्यवाहियों को सार्वजनिक नहीं कर सकते, जबकि न्यायालय की कार्यवाहियाँ खुले न्यायालय (Open Court) में होती है जिससे गोपनीयता नहीं रह पाती।
इसी प्रकार माध्यस्थम (Arbitration) के और भी अनेक लाभ हैं जिसके कारण दिन-प्रतिदिन इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है।
संक्षेप में, माध्यस्थम् एक ऐसा तरीका है जिसमें विवादित पक्षकार आपसी बातचीत और मध्यस्थ की मदद से जल्दी, सरल, सस्ते और शांतिपूर्ण ढंग से अपने मध्य हुए विवाद का निपटारा करते हैं यानि माध्यस्थम् विवाद निवारण का एक प्रभावी, तेज़ और शांतिपूर्ण तरीका है।
इसमें न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि रिश्तों की भी रक्षा होती है। वर्तमान समय में इसे न्यायालयीन प्रक्रिया के विकल्प के रूप में सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है।