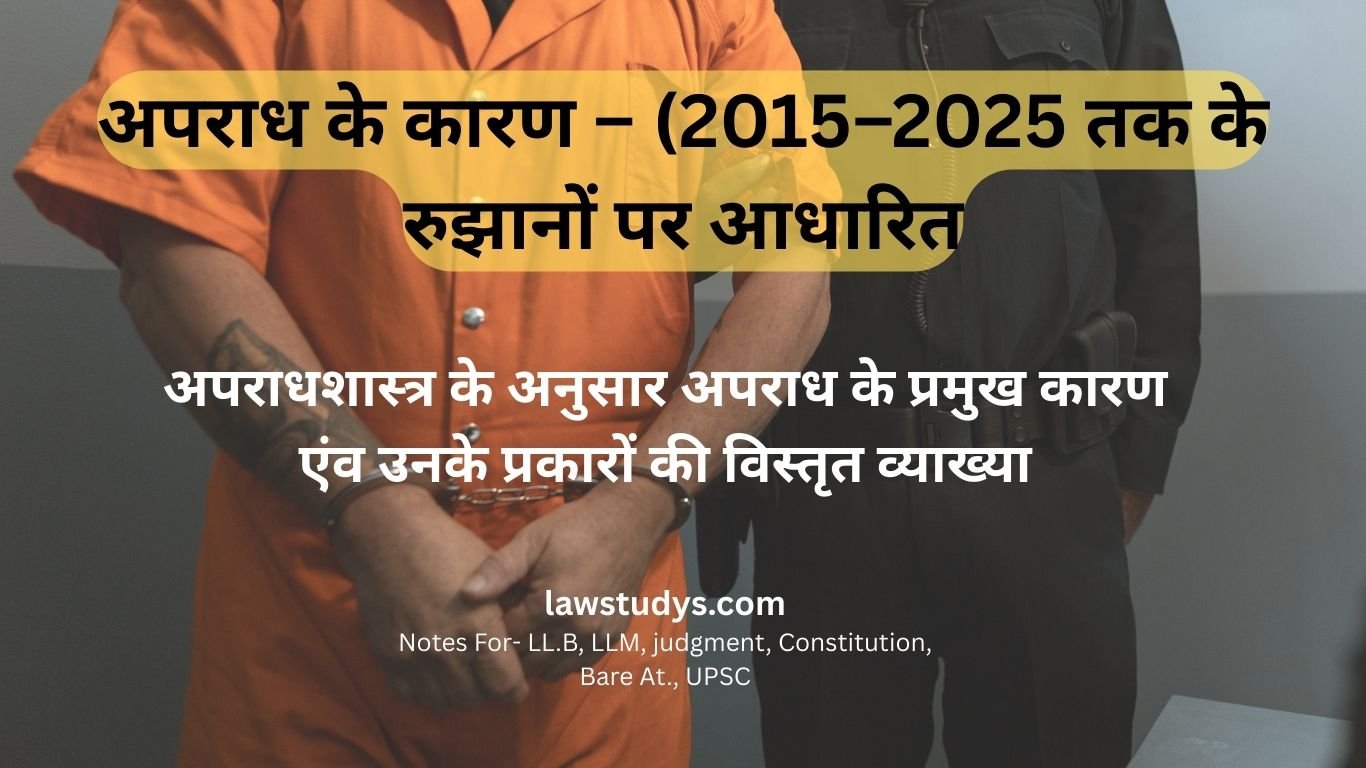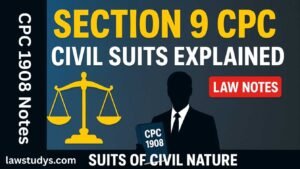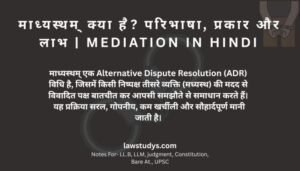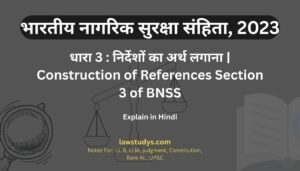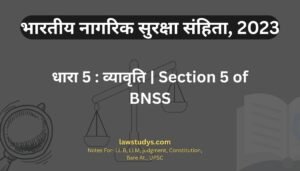अपराध किसी भी समाज के लिए चिंताजनक विषय है। यह न केवल समाज में असुरक्षा पैदा करता है, बल्कि आर्थिक और मानसिक नुकसान भी पहुंचाता है। अपराध के अनेक कारण होते हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और व्यक्तिगत कारण प्रमुख हैं। इस आलेख में अपराध के कारण एंव उनके प्रकारों को विस्तार से समझाया गया है।
परिचय : अपराध के कारण
हमेशा अपराध के पीछे कोई न कोई कारण निहित रहता है, इसे हम आशय या हेतुक कह सकते हैं। अपराधशास्त्र में अपराधों के कारण अलग-अलग बताये गये हैं जो किसी न किसी सम्प्रदाय अथवा विचारधारा (School) पर आधारित हैं। अपराधशास्त्री अपराधों के मुख्यतया निम्नलिखित कारण मानते हैं –
(1) शारीरिक कारण,
(2) पारिवारिक कारण,
(3) सामाजिक कारण,
(4) आर्थिक कारण,
(5) राजनीतिक कारण,
(6) मनोवैज्ञानिक कारण,
(7) अन्य कारण
अपराध के कारण
(1) शारीरिक कारण :
इन्हें वैयक्तिक कारण भी कहा जाता हैं। विख्यात अपराधशास्त्री लोम्ब्रोसो इसके प्रबल समर्थक हैं। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी व्यक्तियों की शारीरिक एवं मानसिक दशा अन्य सामान्य व्यक्तियों से कुछ भिन्न होती है और ऐसा वंशानुगत होता है। इसी आधार पर लोम्ब्रोसो ने जन्मजात अपराधी की अवधारणा को जन्म दिया जिसे एटाविस्ट का नाम दिया गया।
यह भी जाने – प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या हैं? इसका महत्व एंव दर्ज कराने की प्रक्रिया | FIR
शारीरिक कारणों को निम्नांकित उपवर्गों में रखा गया है –
(क) आयु – अपराधों को प्रभावित करने वाला पहला लक्षण अपराधी की आयु है। अपराधशास्त्रियों के अनुसार, 15-16 वर्ष की आयु के व्यक्ति साधारण अपराध कारित करते हैं, जबकि 25-26 वर्ष की आयु के व्यक्ति गम्भीर प्रकृति के अपराध कारित करते हैं। वृद्धावस्था में यौन अपराध अधिक कारित होते हैं। अपराधशास्त्री बर्क इसके समर्थक माने जाते हैं।
(ख) लिंग – अपराधशास्त्रियों की मान्यता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक अपराध कारित करते हैं। पोलक के अनुसार महिलायें अपकर्षण, ठगी, गर्भपात, वेश्यावृत्ति जैसे अपराध कारित करती हैं। समलिंगी सम्भोग की प्रवृत्ति पुरुषों में अधिक पाई जाती है। प्रो. स्मिथ लैंगिक विकृति को भी अपराध के कारण मानते हैं।
(ग) शारीरिक रचना – व्यक्ति की शारीरिक रचना, आकार, बनावट, आकृति आदि भी अपराधों के कारण बनते हैं। सामान्य प्रकृति एवं सौम्य स्वभाव के व्यक्ति कम अपराध करते हैं, जबकि असामान्य प्रकृति के व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक अपराध करते हैं।
कुरूप, विकलांग, बौने व्यक्ति समाज में हेय, घृणा एवं उपहास के पात्र समझे जाते हैं जिनके कारण उनमें कुण्ठा का भाव उत्पन्न हो जाता है और वे अपराध की ओर प्रवृत्त होने लग जाते हैं। अपराधशास्त्री गोरिंग इसके समर्थक माने जाते हैं।
(घ) मानसिक दशा – व्यक्ति की मानसिक दशा भी उसे अपराधों की ओर उन्मुख करती है। मन्द बुद्धि, मनोविक्षिप्त, पागल, जड़, उन्मत्त, विकृत चित्तता आदि विकृत मानसिकता के लक्षण हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक अपराध कारित करते हैं, क्योंकि उनमें कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने की क्षमता नहीं होती है।
जोडार्ड ने अपने परीक्षण से यह साबित किया कि, अपराधी सामान्यतया मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त होते हैं। वे मन्द बुद्धि भी होते हैं। गोरिंग ने भी विभिन्न अपराधियों का बुद्धि परीक्षण कर यह साबित करने का प्रयास किया है कि अपराधी व्यक्ति कम बुद्धि के होते हैं।
अपराधशास्त्री गेरोफेलो के विचार में अपराधी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं और यह प्रवृत्तियाँ वंशानुगत होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती रहती हैं।
यह भी जाने – आरोप की परिभाषा एंव अन्तर्वस्तु | त्रुटिपूर्ण आरोप का प्रभाव | Definition of allegation
डोनाल्ड आर. टेफ्ट ने प्रज्ञा और आपराधिकता में निकट का सम्बन्ध बताते हुए कहा है कि, मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति स्वभाव से आलसी एवं भीरू होते हैं।
उनमें सोचने व समझने की क्षमता भी नहीं होती है, इसीलिए वे प्रकृति एवं परिणामों पर विचार किये बिना अपराध कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति लैंगिक अपराध कम कारित करते हैं क्योंकि उनमें कामवासना का अभाव होता है।
सदरलैण्ड के अनुसार, अपराध के लिए बुद्धिहीनता की बजाऐ बुद्धि की तीव्रता अधिक हैं। उनके अनुसार कुछ अपराधों में बुद्धि की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे- ठगी, कूट रचना, आपराधिक षड्यन्त्र आदि। ऐसे अपराध प्रखर बुद्धि के व्यक्ति योजना बनाकर ही कारित कर सकते हैं।
(2) पारिवारिक कारण :
पारिवार, अपराध के कारण में दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण है। व्यक्ति का आचरण पारिवारिक परिवेश पर अधिक निर्भर करता है। परिवार में व्यक्ति को जैसा वातावरण मिलता है वह वैसा ही आचरण करता है। इसलिए कहा जाता है कि, परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है।
डोनाल्ड आर. टेफ्ट के मतानुसार, परिवार न केवल प्रथम अपितु सर्वाधिक सजातीय, एकीकृत एवं अन्तरंग सामाजिक पाठशाला है।
यह भी जाने – अपकृत्य तथा अपराध मै प्रमुख अंतर | Difference Between Tort And Crime
अपराध के कारण में निम्नांकित पारिवारिक परिस्थितियाँ अधिक उत्तरदायी हैं –
(क) पारिवारिक नियन्त्रण का अभाव,
(ख) परिवार का विघटन,
(ग) परिजनों के प्रति उपेक्षा
(घ) साहचर्य की कमी
(ङ) भावनात्मक तनाव आदि
जिस परिवार में पति-पत्नी में हमेशा झगड़े होते हैं, पिता शराबी या जुआरी होता है, अभिभावक व्यभिचारी होते हैं, परिजन व्यसनी होते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, परिवार में धार्मिक वातावरण नहीं होता है, अत्यधिक भीड़ होती है, कुसंस्कार होते हैं, पारस्परिक साहचर्य का अभाव होता है, उपेक्षावृत्ति का भाव रहता है, माता-पिता में विवाह-विच्छेद हो जाता है, उस परिवार में अपराधों में बढ़ोतरी होनी स्वाभाविक है।
इसी प्रकार जो परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है, जिसमें सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है, पारिवारिक सदस्य बेरोजगार होते हैं, ऐसे परिवारों में चोरी, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार जैसे अपराध कारित करने वाले व्यक्ति होते हैं। आत्महत्या भी ऐसे ही परिवारों में अधिक होती है। बेरोजगारी आत्महत्या के प्रयत्न का प्रमुख कारण है।
इसी प्रकार पारिवारिक विघटन भी अपराधों का एक मुख्य कारण है। अपराधशास्त्री टॉबी के मतानुसार, विघटित परिवार का बच्चों एवं नवयुवतियों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे उनके अपराधी बनने की सम्भावनाएँ प्रबल हो जाती है।
यह भी जाने – बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? इसके कारण तथा उपचार | child crime in Hindi
(3) सामाजिक कारण :
इसी तरह समाज द्वारा कई बार व्यक्ति के साथ किया गया सौतेला एवं उपेक्षित व्यवहार भी उसे अपराधी बना देता है। छोटी-छोटी बातों पर समाज द्वारा समाज के किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है जिससे व्यक्ति में कुण्ठायें पैदा हो जाती है और वह अपराध की ओर कदम बढ़ाने लगता है।
(4) आर्थिक कारण :
जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि- निर्धनता, अर्थाभाव, आर्थिक विषमतायें आदि अपराध के अहम् कारण हैं। जब परिवार आर्थिक संकट में होता है तब परिजन चोरी, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार जैसे अपराधों की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं।
बेकारी एवं बेरोजगारी भी अनेक अपराधों एवं दुष्प्रवृत्तियों की जननी है। बेकार एवं बेरोजगार व्यक्ति चोरी, आवारागर्दी, वेश्यावृत्ति, यौन-शोषण, भिक्षावृत्ति, नशा आदि की ओर बढ़ता है।
मनुष्य में लोभ, प्रलोभन, स्वार्थ एवं अधिक धन अर्जित करने की लालसा भी अपराधों को जन्म देती है। चोरी, लूट, डकैती, आपराधिक न्यास भंग, छल, कपट, तस्करी, कालाबाजारी, मिलावट, रिश्वत आदि अपराध इसी के परिणाम हैं।
अरस्तू के अनुसार, धन अथवा स्वर्ण की लालसा ही अपराधों का मूल कारण है। अधिकांश अपराध मात्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं किये जाकर अतिरिक्त धन या वस्तुयें प्राप्त करने के लिए किये जाते हैं।
प्लेटो भी अपराधों का मुख्य कारण प्रलोभन को मानते हैं। व्यक्ति प्रलोभन में आकर ही अनेक अपराध कर बैठता है।
अपराधशास्त्री प्लेटो, बकारिया के मतानुसार – निर्धनता, भुखमरी आदि से व्यक्ति में निराशा उत्पन्न होती है और वह अपराध कारित करने लगता है।
डोनाल्ड आर. टैफ्ट के अनुसार अर्थाभाव एवं आवश्यकतानुसार वस्तुओं के नहीं मिलने पर व्यक्ति में आर्थिक हीनता का भाव पनपता है और वह अपराधों के द्वारा अर्थाभाव को मिटाने का प्रयास करता है। यह सही है कि, आर्थिक विषमताओं से वर्ग संघर्ष का जन्म होता है और वर्ग संघर्ष अनेक अपराधों का कारण बनता है।
(5) राजनैतिक कारण :
अपराधों के लिए राजनीतिक कारण को भी उत्तरदायी हैं। वर्तमान समय में यह एक आम धारणा बन चुकी है कि अधिकांश अपराधियों को राजनेताओं का संरक्षण मिलता है।
ऐसे व्यक्ति निःसंकोच एवं निडर होकर अपराध करते हैं, क्योंकि शासन व प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे संरक्षण के पीछे राजनेताओं का भी अपना स्वार्थ होता है। चुनाव के समय ऐसे अपराधी राजनेताओं का सहयोग करते हैं, जैसे-
(क) चुनाव में चन्दा अर्थात् आर्थिक सहयोग देना
(ख) मतदाताओं को वोट देने के लिए बल एवं हिंसा द्वारा विवश करना
(ग) मतदाताओं को डराना, धमकाना, भयभीत करना,
(घ) बूथों पर कब्जा करना
(ङ) मतपेटियों को छीनकर ले जाना
(च) फर्जी मतदान कराना, आदि।
यही कारण है कि आजकल राजनीति के अपराधीकरण की बात कही जाती है।
(6) मनोवैज्ञानिक कारण :
अपराधों का मनोवैज्ञानिक कारण भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। अल्फ्रेड बिनेट फ्रांस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए है, उन्होंने अपनी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में निरन्तर प्रयोग करने के पश्चात् व्यक्तियों में पाई जाने वाली मन्द बुद्धि की समस्या के सम्बन्ध में मानसिक आयु तथा प्रज्ञा बुद्धि की संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया और आपराधिकता पर उसके प्रभाव की विवेचना की।
अल्फ्रेड बिनेट की प्रयोगशाला को अमेरिकन मनोवैज्ञानिक प्रो. जर्मन ने आगे बढ़ाया। उनके मत में मानसिक आयु से तात्पर्य बालक की उस अवस्था से है जब उसमें सामान्य बुद्धि का विकास हो जाता है और उसमें कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने की क्षमता आ जाती है।
यह क्षमता आयु के साथ-साथ बढ़ती जाती है, जिसे प्रज्ञा लब्धि कहा जाता है। एक ओर वैज्ञानिक फ्रायड, जिनका इस दिशा में विशेष योगदान माना जाता है, उन्होंने आपराधिकता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए कहा है कि मानव मस्तिष्क में तीन प्रमुख भावनायें सदैव आपस में टकराती रहती है, जिन्हें –
(क) इड,
(ख) इगो,
(ग) सुपर इगो कहा जाता है।
इड से तात्पर्य मानव की उन प्राकृतिक इच्छाओं से है जो उनके जैविक एवं भौतिक अस्तित्व के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का परिवार के लोगों के प्रति स्नेह इड की भावना के कारण होता है।
इगो से तात्पर्य स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति मानव की जागरूकता से है। उदाहरण के लिए भूख, प्यास, सम्भोग की इच्छा आदि मानव स्वभाव की नैसर्गिक क्रियायें हैं।
इन इच्छाओं की पूर्ति मनुष्य वैधानिक साधनों द्वारा ही करना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि अवैध साधनों से की गई पूर्ति समाज में बदनामी का कारण हो सकती है और उससे उसके अहम् को चोट लग सकती है। यह जागरूकता इगो के रूप में जानी जाती है।
जबकि आत्मपरीक्षण एवं संयम की शक्ति की सुपर इगो कहलाती है। जिन व्यक्तियों की सुपर इगो प्रबल होती है वे कभी अपराध कारित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सुपर इगो उन्हें सदैव अपराध से दूर रखती है।
इनके आधार पर अपराधशास्त्री फ्रायड ने यह निष्कर्ष निकाला कि,
(क) अपराध के लिए इड उत्तरदायी है,
(ख) जिस व्यक्ति की इगो तथा सुपर इगो कमजोर होती है वे अक्सर अपराध कारित करते हैं,
(ग) अपराध से बचने के लिए इड अर्थात् भौतिक इच्छाओं पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है तथा
(घ) ऐसा नहीं कर पाने पर व्यक्ति में निराशा आ जाती है, वह क्रोध या सदमे का शिकार हो बैठता है जो कभी-कभी आत्महत्या का कारण बन जाता है।
डोनाल्ड आर. टैफ्ट के अनुसार मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति सामान्यतः आलसी एवं भीरू प्रवृत्ति के होते हैं इसलिये वे अपराध कारित करने से डरते हैं, जबकि प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति अपराध कारित करने से नहीं डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कभी पकड़ में नहीं आयेंगे। ऐसे व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से अपराध कारित करते हैं।
डॉ. ई.ए. ह्यूटन द्वारा भी मानसिक रूप से विकृत अपराधियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया। उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि, प्रायः सभी मापदण्डों के अनुसार मानसिक रूप से विकृत अपराधी सामान्य व्यक्तियों से हीन होते हैं। ऐसे अपराधियों को समाज से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन सदरलैण्ड इस विचार से सहमत नहीं है।
मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आपराधिक प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। उनके अनुसार महिलाओं की अपेक्षा पुरुष इसलिये अधिक अपराध करते हैं क्योंकि उन्हें परिवार को पालना होता है तथा संरक्षण प्रदान करना होता है, जबकि महिलाओं को आदर्श गृहिणी की भूमिका निभानी होती है।
परिवार में भी लड़कियों से शालीन, विनम्र एवं सदाचारी बनने की अपेक्षा की जाती है, जबकि लड़कों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतन्त्र रहें, किसी से डरे नहीं, दबे नहीं और सदैव पौरुषता का परिचय दें। यही शिक्षा पुरुषों को अपराधी बना देती है।
मनोवैज्ञानिक अपराधों के निम्नांकित कारण हैं-
(क) भावनात्मक अस्थिरता,
(ख) हीनता की भावनाय,
(ग) पारिवारिक वातावरण
भावनात्मक अस्थिरता वाले लोग सही और सामयिक निर्णय नहीं ले पाते हैं जिससे वे अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हीनता की भावना वाले व्यक्ति मानसिक सन्तुलन खो बैठते हैं और वे भय, क्रोध, नफरत आदि से ग्रसित हो जाते हैं जो उन्हें अपराधी बनाने का कारण बनता है। पारिवारिक विघटन एवं वातावरण भी अपराधों का एक अहम् कारण है।
मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति अधिक अपराध कारित करते हैं, जो-
(i) भावनात्मक तौर पर कमजोर होते हैं,
(ii) आर्थिक रूप से विपन्न एवं असुरक्षित होते हैं,
(iii) आजीविका के लिए सदैव संघर्षरत रहते हैं,
(iv) बेकार एवं बेरोजगार होते हैं,
(v) पारिवारिक कलह से पीड़ित होते हैं,
(vi) किसी प्रेम प्रसंग में निराश हो जाते हैं,
(vii) किसी अप्रिय घटना के शिकार हो जाते हैं,
(viii) शिशु काल से ही निराश होते हैं।
(7) अन्य अपराध के कारण :
ऊपर वर्णित कारणों के अलावा भी अपराध के कारण ओर भी हैं, जो निम्नाकिंत है-
(क) अश्लील साहित्य,
(ख) सिनेमा, दूरदर्शन, इन्टरनेट एवं अश्लील फिल्में,
(ग) सह-शिक्षा,
(घ) नैतिक एवं चारित्रिक पतन आदि।
निष्कर्ष
अपराध केवल किसी व्यक्ति की ही गलती नहीं होती है, बल्कि यह कई सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न होता है। अपराध को रोकने के लिए समाज में शिक्षा, सामाजिक सुधार लाना तथा मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता भी आवश्यक है।
महत्वपूर्ण आलेख
दण्ड न्यायालयों के वर्ग और उनकी शक्तियों की विवेचना | Sec. 6 of BNSS in Hindi
1726 का चार्टर एक्ट: भारतीय कानूनी इतिहास की शुरुआत
प्रशासनिक कानून : शासन व्यवस्था की रीढ़ – परिभाषा, प्रकृति एवं उसके विस्तार क्षेत्र की व्याख्या