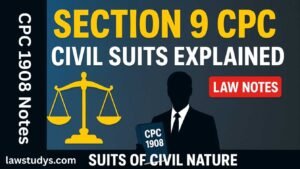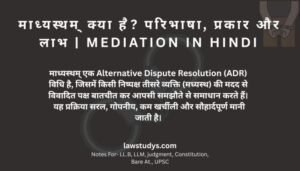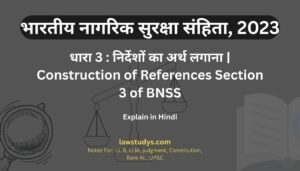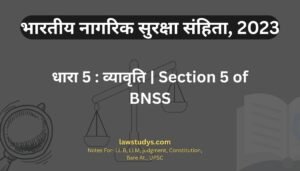इस आलेख में विधि व्यवसाय क्या है? परिभाषा एंव भारत इसका विकास किन-किन चरणों में हुआ का विस्तृत वर्णन किया गया है, यह आलेख विधि के छात्रो के काफी उपयोगी है, इसे अन्त तक जरुर पढ़े, धन्यवाद-
विधि एक जटिल विषय हैं इसकी भाषा एवं उपबन्ध को अत्यधिक कठिन माना जाता हैं। विधि को समझ पाना हर व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है।
योग्य, अनुभवी एवं प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही इसे आसानी से समझ सकता हैं। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में विधि का अपना एक अलग ही पाठ्यक्रम है और जो व्यक्ति यह पाठ्यक्रम करता है वह व्यक्ति अधिवक्ता (Advocate) कहलाता है।
परिचय – विधि व्यवसाय
अधिवक्ता का कार्य न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकार के पक्ष को प्रस्तुत करना तथा उसकी ओर से पैरवी करना होता है। एक तरह से यह उसका व्यवसाय है, क्योंकि इसके एवज में वह अपने पक्षकार से शुल्क प्राप्त करता है और यही व्यवसाय ‘विधिक व्यवसाय’ अथवा ‘विधि व्यवसाय’ (Legal profession) कहलाता है। विधि व्यवसायी को अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील, प्लीडर आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके साथ ही विधि व्यवसाय की अपनी कुछ विशेषताऐं भी होती है|
यह भी जाने – अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) क्या है? यह कब और कैसे मिलती है | CrPC in Hindi
विधि व्यवसाय की विशेषताऐं
(i) यह एक स्वतन्त्र एवं पवित्र व्यवसाय है।
(ii) इसका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।
(iii) जो व्यक्ति यह व्यवसाय करता है वह अधिवक्ता कहलाता है।
(iv) इस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है सेवा भावना।
(v) इस व्यवसाय को करने वाले व्यक्तियों के समूह को बार (Bar) कहा जाता है।
(vi) बार एवं बैंच के बीच मधुर सम्बन्धों की परिकल्पना की जाती है।
(vii) इसमें दलाली अथवा भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है।
(viii) विधि व्यवसायी न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं।
भारत में विधिक व्यवसाय का विकास
भारत में विधिक व्यवसाय की जड़ें अतीत की गहराईयों में छिपी हैं। सामान्यतः भारत में इसका श्रीगणेश ब्रिटिश काल से माना जाता है। इससे पूर्व विधिक व्यवसाय जैसी कोई बात भारत में नहीं थी।
हिन्दू काल में इसका अस्तित्व नहीं था, क्योंकि राजा ही न्यायाधीश (Fountain of justice) हुआ करता था। वहाँ किसी प्रकार की विधिक औपचारिकतायें नहीं हुआ करती थीं।
भारत में विधिक व्यवसाय के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन हम निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते है –
यह भी जाने – विधि का शासन: परिभाषा, डायसी का सिद्धांत और भारतीय संविधान में महत्व
(1) मेबर कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधीन विधि व्यवसाय
भारत में विधिक व्यवसाय का सूत्रपात मेयर कोर्ट की स्थापना से माना जा सकता है। ब्रिटिश भारत में सन् 1926 के चार्टर द्वारा प्रथम बार मेयर न्यायालयों की स्थापना की गई। इन न्श्यायालयें में न्याय प्रशासन का संचालन एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता था। इन न्यायालयों का गठन एवं प्रक्रिया इंग्लैण्ड के न्यायालयों के समान थी।
इस चार्टर (Charter) में तथा आगे के कुछ अन्य चार्टरों में विधिक व्यवसाय को स्थान दिया गया था। लेकिन इस व्यवसाय को व्यवस्थित स्वरूप सन् 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट तथा सन् 1774 के चार्टर द्वारा प्रदान किया गया। इन्हीं के अन्तर्गत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
(2) कम्पनी न्यायालयों में विधि व्यवसाय
यद्यपि मेयर कोर्ट की स्थापना के साथ ही विधिक व्यवसाय का सूत्रपात हो गया था लेकिन वह नियमित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त नहीं कर सका। सन् 1793 में एक रेगूलेशन पारित किया गया जिसमें बंगाल में सदर दीवानी अदालत के लिए वकीलों को प्रथम बार सूचीबद्ध किया गया।
कालान्तर में सन् 1814 के बंगाल रेगूलेशन में विधिक व्यवसाय के सम्बन्ध में कतिपय उपबन्ध किये गये जिन्हें सन् 1833 के रेगूलेशन द्वारा परिष्कृत किया गया।
यह भी जाने – निर्धन व्यक्ति कौन है और वाद दायर करने की प्रक्रिया | Order 33 CPC
(3) भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अधीन विधिक व्यवसाय
सन् 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम (Indian High Courts Act) पारित किया गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रेसीडेन्सी नगर में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं सदर अदालतों का अवसान कर दिया गया।
इस अधिनियम तथा अन्य चार्टरों द्वारा उच्च न्यायालयों को वकील, एटार्नी, एडवोकेट आदि को सूचीबद्ध करने तथा अनुमोदित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई। इन न्यायालयों में सूचीबद्ध व्यक्तियों को ही वकालत करने का अधिकार था।
(4) लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट के अधीन विधि व्यवसाय
विधिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट (Legal. Practioner’s Act) पारित किये गये, यथा-लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट, 1846, लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट, 1853, लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट 1879 आदि।
सन् 1846 के एक्ट के अनुसार केवल सूचीबद्ध वकील ही न्यायालयों में प्रेक्टिस कर सकते थे। सन् 1853 के एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एटार्नी तथा बैरिस्टर को कम्पनी की सदर अदालतों में अभिवचन करने की इजाजत प्रदान की गई, लेकिन भारतीय वकील सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकते थे।
सन् 1879 के एक्ट द्वारा विधि व्यवसायियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया- (i) एडवोकेट, एवं (ii) वकील।
एडवोकेट आयरलैण्ड या इंग्लैण्ड का बैरिस्टर या स्कॉटलैण्ड के प्लीडर संकाय का सदस्य होता था जबकि वकील भारतीय विश्वविद्यालयों के विधि स्नातक हुआ करते थे।
(5) इण्डियन बार कौंसिल एक्ट, 1926 के अधीन विधि व्यवसाय
सन् 1923 में सर एडवर्ड चामियार की अध्यक्षता में एक इण्डियन बार कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को निम्नांकित के बारे में सुझाव देने का काम सौंपा गया –
(i) बार का गठन, तथा
(ii) हाईकोर्ट के लिए अखिल भारतीय स्तर पर बार कौंसिल की स्थापना।
इस कमेटी द्वारा विभिन्न सुझाव दिये गये जिनमें से एक विधि व्यवसाय का एक ही वर्ग रखे जाने के बारे में था और ऐसे विधि व्यवसायी को एडवोकेट नाम दिया जाना था।
कमेटी के सुझावों को लागू करने के लिए सन् 1926 में इण्डियन बार कौंसिल एक्ट पारित किय गया। लेकिन यह एक्ट भी सार्थक नहीं रहा। मुफस्सिल कोर्ट में कार्य करने वाले वकील एवं मुख्तार इस एक्ट की परिधि में नहीं आते थे।
(6) स्वतन्त्र भारत में विधि व्यवसाय
विधि व्यवसाय को संगठित एवं व्यवस्थित स्वरूप स्वतन्त्र भारत में मिला। सन् 1951 में न्यायमूर्ति एस. आर. दास की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय विधिक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी द्वारा निम्नांकित की स्थापना करने का सुझाव दिया गया –
(i) भारतीय विधिज्ञ परिषद् (Bar Council of India); तथा
(ii) राज्य विधिज्ञ परिषद् (State Bar Council)
कमेटी ने इन परिषदों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की सिफारिश की।
इसी अनुक्रम में सन् 1961 में अधिवक्ता अधिनियम (Advocate Act, 1961) पारित किया गया। इस अधिनियम में अधिवक्ताओं की आचार संहिता, पंजीयन, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, राज्य विधिज्ञ परिषद् आदि के बारे में विस्तृत व्यवस्था की गई है। अब भारत में विधि व्यवसायियों का एक संगठित एवं सुव्यवस्थित समूह है।
विधि व्यवसाय करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
अब हम जानेगें की विधि व्यवसाय करने का अधिकार किसे है अथवा अधिवक्ता के पास विधि व्यवसाय के लिए कोनसे अधिकार होते है?
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि “विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों का एक वर्ग होगा अर्थात् अधिवक्ता।” इससे स्पष्ट है कि विधि व्यवसाय करने का हक केवल अधिवक्ताओं (Advocates) को है, अन्य किसी को नहीं।
एन. राम रेड्डी बनाम बार कॉसिल ऑफ स्टेट, आंध्र प्रदेश (ए.आई. आर. 2002 आंध्र प्रदेश 484) के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि- “अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय करने का अधिकार मात्र एक सांविधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं।” कुछ भी हो, विधि व्यवसाय का अधिकार केवल अधिवक्ता वर्ग को प्राप्त है, अन्य किसी व्यक्ति या वर्ग को नहीं।
अधिनियम की धारा 30 में यह उपबन्ध किया गया है कि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ता नामावली (Roll of Advocates) में अंकित हैं –
(i) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में,
(ii) किसी न्यायाधिकरण (Tribunal) अथवा साक्ष्य लेने हेतु विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष, और
(iii) ऐसे किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के समक्ष, जहाँ कोई अधिवक्ता तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए अधिकृत हो, विधि व्यवसाय करने का हकदार है।
बलराज सिंह मलिक बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (ए.आई.आर. 2012 दिल्ली 79) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने समक्ष वकालत करने तथा कार्य करने बाबत नियम बना संकता है। वह वकालत करने की शर्ते भी तय कर सकता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार केवल अधिवक्ताओं को ही है बशर्ते कि उनका नाम विधिज्ञ परिषद् की अधिवक्ताओं की नामावली में प्रविष्ट हो।
अधिनियम की धारा 33 में भी यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा जिसका नाम इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट न किया गया हो।
* इसी प्रकार अधिनियम की धारा 45 में यह और प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं है, किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विधि व्यवसाय करता है तो उसका यह कृत्य अवैधानिक माना जाएगा और उसे छः माह तक की अवधि के कारावास से दण्डित किया जा सकेगा।
इस सम्बन्ध में नीलगिरी बार एसोसिएशन बनाम टी. के. महालिंगम (1998 क्रि. लॉ रि. 247 एस. सी.) का एक अच्छा प्रकरण है। इसमें प्रत्यर्थी के पास न तो विधि स्नातक की उपाधि थी और न ही उसका नाम अधिवक्ता की नामावली में अंकित था, फिर भी वह लगातार 8 वर्षों तक न्यायालयों में वकालत करता रहा। जब उसे अभियोजित किया गया तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया।
विचारण न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध ठहराते हुए परिवीक्षा (Probation) का लाभ दिया। उच्च न्यायालय द्वारा भी परिवीक्षा के आदेश को यथावत् रखा गया। लेकिन जब मामला उच्चतम न्यायालय में पहुँचा तो उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यर्थी को 6 माह के कठोर कारावास एवं 5000/- रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। जुर्माना जमा नहीं कराए जाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया।
न्यायालय ने कहा- “विधि व्यवसाय एक पवित्र एवं आदर्श व्यवसाय है। अधिवक्ताओं का समाज में विशिष्ट स्थान भी है। जनसाधारण में अधिवक्ताओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसो स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाने वाला कोई कार्य करता है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं रह जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कठोर दण्ड ही उचित दण्ड है।”
ऐसा ही एक और मामला राजेन्द्र सिंह बनाम डॉ. सुरेन्द्र सिंह (1992 क्रि. ला. ज. 3749 मध्रूप्रदेश) का है। इस मामले में मध्रूप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “विधि व्यवसाय एक आदर्श व्यवसाय है।
अधिवक्ता को गरिमा, शालीनता एवं अनुशासन के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। अधिवक्ताओं की अपनी एक आचार संहिता (Code of conduct) भी है। कोई भी व्यक्ति तब तक विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है जब तक उसके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न हो और अधिवक्ता की नामावली में उसका नाम प्रविष्ट न हो।
यदि कोई व्यक्ति जिसके पास न तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है और न ही उसका नाम अधिवक्ता की नामावली में प्रविष्ट है, विधि व्यवसाय करता है तो उसे अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।”
‘लक्ष्मीनारायण बनाम बार कौंसिल ऑफ इण्डिया’ (ए.आई.आर. 1999 राजस्थान 325) के मामले में ऐसे व्यक्ति को अधिवक्ता की नामावली में नाम प्रविष्ट कराने का हकदार माना गया है जो विधि स्नातक है तथा किसी विश्वविद्यालय में विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत है।
इसी प्रकार परमानन्द शर्मा बनाम बार कौंसिल ऑफ राजस्थान (ए.आई.आर. 1999 राजस्थान 171) के मामले में ऐसे व्यक्ति को विधिज्ञ परिषद् की नामावली में नाम प्रविष्ट कराने का हकदार माना गया है जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा हो।
सुरेन्द्रराज जारूपवाल बनाम श्रीमती विजय जारूपवाल (ए.आई.आर. 2003 आंध्र प्रदेश 317) के मामले में एक अत्यन्त रोचक प्रश्न उठा कि क्या अधिवक्ता से भिन्न कोई व्यक्ति न्यायालय की अनुज्ञा से किसी प्रकरण विशेष में उपस्थिति दे सकता हैं? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि यह अधिवक्ता के विधि व्यवसाय करने के अधिकार का एक अपवाद है।
ऐसे व्यक्ति जो विधि व्यवसाय नहीं कर सकते –
पूर्व में हमने जाना कि विधि व्यवसाय के लिए दो बातें आवश्यक हैं –
(i) विधि स्नातक होना, तथा
(ii) अधिवक्ताओं की नामावली में नाम दर्ज होना।
लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यवसाय, व्यापार या कारोबार में लिप्त या संलग्न है वह व्यक्ति विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है।
इस सम्बन्ध में डॉ. हनीराज एल चुलानी बनाम बार कौंसिल ऑफ महाराष्ट्र (ए.आई.आर. 1996 एस. सी. 2076) का एक अच्छा मामला है। इसमें उचचतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि “विधि व्यवसाय एक पूर्णकालिक व्यवसाय है। अधिवक्ताओं को अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होकर कार्य करना होता है। उन्हें अपने पक्षकारों को पूरा समय भी देना होता है।
इसलिए यह आवश्यक है कि कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय करता है तो वह अपने पक्षकारों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।” इस मामले में अपीलार्थी एक चिकित्सक था और वह अपना नाम अधिवक्ताओं की नामावली में प्रविष्ट कराना चाहता था।
इसी प्रकार शेख महबूब हुसैन बनाम सेक्रेटरी बार कौंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश (ए.आई.आर. 2003 एन. ओ. सी. 295 आंध्र प्रदेश) के मामले में ऐसे व्यक्ति को विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं माना गया है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17ख के अन्तर्गत अपने नियोक्ता से पूर्ण पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रबन्धक के अधीन नियोजन में माना जाता है।
ऐसा ही एक और मामला डॉ. सांई बाबा बनाम बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर. 2003 एस. सी. 2502) का है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो एस. टी. डी. बूथ चला रहा है, तब तक विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं माना गया है जब तक वह एस. टी. डी. बूथ को समर्पित (Surrender) नहीं कर देता अर्थात् वह इस व्यवसाय को छोड़ नहीं देता।
को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल बैंक लि. बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (ए.आई.आर. 2003 कर्नाटक 30) के मामले में न्यायालय में पैरवी करने के लिए वकालतनामे (Vakalatnama) को आवश्यक माना गया है। वकालतनामे के अभाव में केवल न्यायालय की अनुज्ञा से ही पैरवी की जा सकती है।
एस. नागन्ना बनाम कृष्णमूर्ति (ए.आई.आर. 1965 आंध्र प्रदेश 320) के मामले में सहायक लोक अभियोजक (APP) को विधि व्यवसाय का हकदार नहीं माना गया है क्योंकि वह राज्य की पूर्णकालिक सेवा में होता है।
इसी तरह जो अधिवक्ता मामले में स्वयं एक पक्षकार है, को न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने का हकदार नहीं माना गया है|
निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार केवल अधिवक्ता वर्ग को ही है, अन्य किसी वर्ग को नहीं। अधिवक्ता ऐसा हो
(i) जिसके पास विधि स्नातक की उपाधि हो, तथा
(ii) जिसका नाम अधिवक्ता की नामावली में प्रविष्ट हो।
इसके बावजूद भी हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई. आर. 2003 एस. सी. 739) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि “अधिवक्ताओं का न्यायालय में उपस्थिति देने तथा पैरवी करने का अधिकार अबाध नहीं है।
न्यायालय का अवमान करने, गैर वृतिक व्यवहार करने या अनपेक्षित आचरण किए जाने पर किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से वंचित करने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं।”
महत्वपूर्ण आलेख
दोहरे खतरे से संरक्षण का सिद्धान्त और इसके प्रमुख अपवाद | Double Jeopardy
लोकहित वाद से आप क्या समझते हैं ? लोकहित वाद का अर्थ, विस्तार एवं उद्देश्य की विस्तृत विवेचना
अधिवक्ता कोन होता है? परिभाषा, प्रकार एंव एक सफल अधिवक्ता के गुण