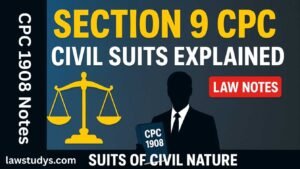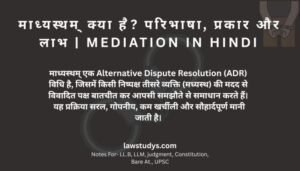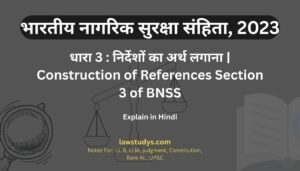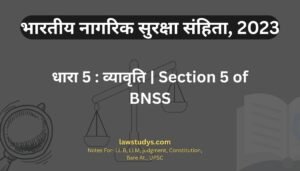इस आलेख में माध्यस्थम् कार्यवाहियों के संचालन एवं समापन सम्बन्धी नियम के बारे में बताया गया है, इसमें मध्यस्थ की नियुक्ति, प्रक्रिया, सुनवाई, निर्णय, पंचाट (Award) और समापन के तरीको का विस्तार से उल्लेख किया गया है –
परिचय : माध्यस्थम् कार्यवाही
विवादों के निपटारे के लिए सामान्यत न्यायालय की प्रक्रिया लंबी, महंगी और जटिल होती है, इसलिए विवादों के समाधान के वैकल्पिक साधनों (Alternative Dispute Resolution – ADR) में माध्यस्थम् (Arbitration) को विशेष महत्व दिया गया है।
माध्यस्थम् एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार अपने विवादों का समाधान न्यायालय से बाहर, किसी निष्पक्ष मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा कराते हैं। लेकिन इसके संचालन के लिए कुछ नियम और प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ताकि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता और जल्दी न्याय शुलभ हो सके।
माध्यस्थम् कार्यवाही का संचालन :
माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 18 से 27 तक में माध्यस्थम् कार्यवाहियों के संचालन सम्बन्धी नियमों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है –
यह भी जाने – भारतीय दण्ड संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है? यह संहिता भारत में कब लागू हुई?
(1) स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कार्यवाही (धारा 18):
माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 18 इस बात पर जोर देती है कि, माध्यस्थम् कार्यवाहियों में सभी पक्षकारों के साथ समानता का व्यवहार किया जाकर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाए।
पक्षकारों के मध्य विवाद के निपटारे के लिए माध्यस्थ को स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कदाचरण (Misconduct) का दोषी न बने तथा पक्षकारों की अनुपस्थिति में भी कोई कार्य ना करे क्योंकि माध्यस्थ, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कार्यवाहियों का मूल मन्त्र है।
(2) नियमों की अवधारणा (धारा 19):
अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत माध्यस्थम् कार्यवाहियों के संचालन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का अधिकार पक्षकारों को दिया गया है। पक्षकार आपस में करार द्वारा प्रक्रिया के नियम तय कर सकते हैं, जिनका माध्यस्थ अधिकरण द्वारा अनुसरण किया जाना आवश्यक है।
यदि पक्षकारों द्वारा प्रक्रिया के नियम तय नहीं किये जाते हैं तो माध्यस्थ अधिकरण द्वारा कार्यवाहियों का संचालन ऐसी रीति से किया जा जायेगा जैसा वह उचित समझे।
माध्यस्थम् कार्यवाहियों के संचालन पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं। इसमें केवल मात्र नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों (Principles of Natural justice) का अनुसरण किया जाना आवश्यक है।
यह भी जाने – बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? इसके कारण तथा उपचार | child crime in Hindi
केस : पी.आर. शाह, शेयर्स एण्ड स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड बनाम मै.बी.एच. एच. सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 1866)
इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि, माध्यस्थ को कार्यवाही के दौरान विवाद बाबत अपनी निजी जानकारी का उपयोग नहीं करना चाहिये जबकि वह किसी व्यापार-विशेष के सम्बन्ध में अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर सकता है।
माध्यस्थम् अधिकरण के पास साक्ष्य की ग्राह्यता, सुसंगतता, तात्त्विकता एवं महत्त्व आदि को अवधारण करने की शक्तियाँ होती हैं। न्यायालय द्वारा इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
(3) माध्यस्थम् का स्थान (धारा 20):
विवाद को निपटाने का स्थान कोनसा होगा यह सुनिश्चित करने का पहला अधिकार पक्षकारों को दिया गया है। पक्षकार करार द्वारा माध्यस्थम् का स्थान तय कर सकते हैं, यदि किसी कारणवश पक्षकार ऐसा करने में असफल रहते हैं तो माध्यस्थम् अधिकरण (i) पक्षकारों की सुविधा; एवं (ii) मामले की परिस्थितियाँ के आधार पर माध्यस्थम् का स्थान सुनिश्चित कर सकता है।
इसके अलावा माध्यस्थ अधिकरण द्वारा निम्नांकित प्रयोजनों के लिए भी किसी भी स्थान पर बैठकें आयोजित की जा सकती हैं –
(क) सदस्यों से परामर्श करने के लिए;
(ख) साक्षियों, विशेषज्ञों एवं पक्षकारों को सुनने के लिए;
(ग) दस्तावेजों, चीजों, सम्पत्तियों आदि का निरीक्षण करने के लिए; आदि।
यह भी जाने – समन क्या होता है और इसे तामील कैसे किया जाता है? | आसान भाषा में समन की प्रक्रिया
माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जो भी स्थान तय किया जायेगा उसकी सूचना पक्षकारों को दिया जाना आवश्यक है और यदि पक्षकार ऐसे स्थान से संतुष्ट नहीं है, तब माध्यस्थ द्वारा पक्षकारों की सुविधा के लिए माध्यस्थम् के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है।
(4) कार्यवाहियों का प्रारम्भ (धारा 21):
अधिनियम की धारा 21 में माध्यस्थम् कार्यवाहियों के प्रारम्भ की तिथि के बारे में प्रावधान किया गया है, इसके अनुसार यदि माध्यस्थम् करार में माध्यस्थम् कार्यवाहियों के प्रारम्भ की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है तो माध्यस्थम् कार्यवाहियों को प्रारम्भ उस तिथि से माना जायेगा जिस तिथि पर माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किये जाने वाले उस विवाद के सन्दर्भ की सूचना माध्यस्थ को प्राप्त होती है।
(5) भाषा (धा 22):
माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाहियों में भाषा वही होगी जो पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जावे, लेकिन किसी कारण से ऐसा करार नहीं होता है तो भाषा का अवधारण माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जायेगा और भाषा ऐसी होगी जिसे माध्यस्थ एंव विवाद के पक्षकार समझते हो।
‘ई. रोथरे एण्ड संस बनाम कार्लो बेडरीडा एण्ड क.’ [(1961) 1 लायड्स रिपोर्ट 220] के मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि यदि कोई दस्तावेज विदेशी भाषा में है जिसे माध्यस्थ नहीं समझते हैं तो ऐसे दस्तावेज का उस भाषा में अनुवाद किया जाएगा जिसे माध्यस्थ समझता हो।
यह भी जाने – पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण से सम्बन्धित प्रावधान : धारा 125 सीआरपीसी 1973
(6) दावा या प्रतिरक्षा के कथन (धारा 23):
अधिनियम की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया है कि –
(i) दावाकर्ता का यह कर्त्तव्य है कि वह निर्धारित कालावधि में अपने दावे का समर्थन करने वाले तथ्यों, विवादित बिन्दुओं और वांछित अनुतोष या उपचार का कथन करे और इसी प्रकार प्रतिवादी दावे की विशिष्टियों के सम्बन्ध में अपनी प्रतिरक्षा का कथन करें;
(ii) पक्षकारों का यह भी कर्तव्य है कि वे अपने दावे या प्रतिरक्षा के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें; तथा प्रत्यर्थी भी अपने मामले के समर्थन में प्रतिदावा प्रस्तुत कर सकेगा या सुनवाई का अभिवाक कर सकेगा जिसका न्याय निर्णयन, यदि ऐसा प्रतिदावा या ऐसी मुजराई माध्यस्थम करार की परिधि के अन्तर्गत आती है, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जायेगा। [ माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा अन्तःस्थापित ]
(iii) पक्षकार आवश्यकतानुसार दावे या प्रतिरक्षा में संशोधन के लिए आवेदन करें। लेकिन संशोधन की अनुमति देना या न देना माध्यस्थम् अधिकरण के विवेक पर निर्भर करता है तथा संशोधन की अनुमति मामले के किसी भी प्रक्रम पर दी जा सकती है।
(7) सुनवाई (धारा 24) :
अधिनियम की धारा 24 सुनवाई एवं लिखित कार्यवाहियों के बारे में प्रावधान करती है, इसके अनुसार माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा यह विनिश्चित किया जायेगा कि साक्ष्य की प्रस्तुती के लिए मौखिक सुनवाई की जाये या मौखिक बहस की जाये या कार्यवाहियों का संचालन दस्तावेजों एवं अन्य सामग्रियों के आधार पर किया जाये।
पक्षकारों के बीच अन्यथा करार नहीं होने पर किसी पक्षकार की प्रार्थना पर मौखिक सुनवाई की जा सकेगी। जहाँ माध्यस्थम् अधिकरण को दस्तावेजों, मालों या सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए बैठक आयोजित करना हो, वहाँ ऐसी बैठक की सूचना पक्षकारों को दी जायेगी।
पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कथनों, दस्तावेजों, आवेदन पत्रों, विशेषज्ञों की रिपोर्टों, साक्ष्यात्मक दस्तावेजों आदि से पक्षकारों को अवगत कराया जायेगा।
माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा सुनवाई दिन-प्रतिदिन की जायेंगी तथा पर्याप्त हेतुक के बिना स्थगम् मंजूर नहीं किया जायेगा और बिना पर्याप्त कारण के स्थगन खर्चे पर मंजूर किया जा सकेगा। [ माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा अन्तःस्थापित ]
केस : दामोदर प्रसाद गुप्ता बनाम सक्सेना एण्ड कम्पनी (ए.आई.आर. 1959 पंजाब 476)-
इस मामले में यह कहा गया है कि ,पक्षकारों को माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है और उन्हें सुनवाई के स्थान एवं समय की सूचना भी पाने का अधिकार है। यदि पक्षकारों को इन अधिकारों से वंचित कर पंचाट जारी किया जाता है तो वह अपास्त किये जाने योग्य होगा।
यदि माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा विवाद के साक्षियों को सुनने का वचन देकर उन्हें नहीं सुना जाकर पंचाट जारी किया जाता है, तो वह संहिता की धारा 24 के तहत अपास्त योग्य है।
(8) एक-पक्षीय कार्यवाही (धारा 25):
संहिता की धारा 25 प्रावधान करती है कि, जहाँ दावाकर्ता दावे के अपने कथनों की संसूचना देने में असफल रहता है या माध्यस्थ द्वारा सूचना देने के पश्चात् भी पक्षकार उपस्थित नहीं रहते हैं तो माध्यस्थ को उनके विरुद्ध माध्यस्थम् कार्यवाहियों को समाप्त एक-पक्षीय कार्यवाही करने का अधिकार है।
जहाँ प्रत्यर्थी धारा 23(1) के अनुसार प्रतिरक्षा का अपना कथन संसूचित करने में असफल रहता है, माध्यस्थम् अधिकरण दावेदार द्वारा अभिकथन की स्वीकृति के रूप में स्वयं उस असफलता को माने बिना कार्यवाहियों को चालू रखेगा और प्रत्यर्थी के ऐसे प्रतिरक्षा कथन को फाइल करने के अधिकार को उस रूप में मानने का विशेषाधिकार होगा मानो कि वह समपहृत हो गया हो।
तथा जहाँ एक पक्षकार मौखिक सुनवाई पर उपसंजात होने या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहाँ माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा कार्यवाहियों को चालू रखते हुए। अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पंचाट निर्मित किया जा सकेगा।
संहिता की धारा 25 (क) के अन्तर्गत माध्यस्थम् अधिकरण को कार्यवाहियों को समाप्त करने तथा पर्याप्त आधार होने पर ऐसे आदेश को पुनः निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है।
(9) विशेषज्ञों की नियुक्ति (धारा 26):
पक्षकार के विवादों को सही तरह से निपटाने के लिए माध्यस्थ अधिकरण संहिता की धारा 26 के अन्तर्गत मामले से सम्बंधित विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते है। पक्षकारों का यह दायित्व होगा कि वे विशेषज्ञों को सुसंगत सूचनायें दें, निरीक्षण के लिए दस्तावेज, माल या सम्पत्ति प्रस्तुत करें तथा विशेषज्ञों को वहाँ तक पहुँचने दें।
(10) साक्ष्य ग्रहण करने में न्यायालय की सहायता (धारा 27):
अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत माध्यस्थ अधिकरण या माध्यस्थ कार्यवाही के पक्षकार साक्ष्य लेने या साक्ष्य देने में न्यायालय की सहायता ले सकते हैं। इसके लिए माध्यस्थम् अधिकरण या अधिकरण के अनुमोदन से एक पक्षकार को साक्ष्य ग्रहण करने में सहायता के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करना होगा। आवेदन-पत्र में निम्नांकित बातों का उल्लेख किया जायेगा-
(i) पक्षकारों तथा मध्यस्थों के नाम व पते,
(ii) दावे की सामान्य प्रकृति तथा चाहा गया अनुतोष; तथा
(iii) प्राप्त किया जाने वाला साक्ष्य आदि।
माध्यस्थम् कार्यवाही का समापन :
माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 32 में माध्यस्थम् कार्यवाहियों के समापन (Terimination of arbitral proceedings) के बारे में प्रावधान किया गया है, इसके अनुसार-
(1) माध्यस्थम् कार्यवाहियाँ या तो अन्तिम माध्यस्थम् पंचाट द्वारा या उपधारा (2) के अन्तर्गत माध्यस्थम् अधिकरण के द्वारा समाप्त हो जायेगी।
(2) माध्यस्थम् अधिकरण माध्यस्थम् कार्यवाहियों की समाप्ति के लिए आदेश वहाँ जारी करेगा जहाँ-
(क) दावाकर्ता अपने दावे का प्रत्याहरण कर लेता है, जब तक प्रत्यर्थी आदेश पर आपत्ति नहीं करता है और माध्यस्थम् अधिकरण विवाद के अन्तिम हल को प्राप्त करने में अपनी ओर से वैध हित को मान्यता नहीं देता है;
(ख) पक्षकारगण कार्यवाहियों की समाप्ति का करार करते हैं; या
(ग) माध्यस्थम् अधिकरण यह पाता है कि कार्यवाहियों का जारी रहना किसी अन्य कारण से अनावश्यक अथवा असम्भव हो गया है।
( 3) धारा 33 और धारा 34 की उप धारा (4) के अध्यधीन रहते हुए माध्यस्थम् अधिकरण का आदेश माध्यस्थम् कार्यवाहियों की समाप्ति के साथ समाप्त हो जायेगा।
धारा 32 के उपबन्धों के अनुसार माध्यस्थम् कार्यवाहियाँ निम्नांकित अवस्थाओं में समाप्त हो जाती हैं-
(1) अन्तिम माध्यस्थम् पंचाट द्वारा:
धारा 32 (1) के अनुसार माध्यस्थम् कार्यवाहियों का समापन निम्नांकित दो दशाओं में हो जाता है-
(i) जब अन्तिम माध्यस्थम् पंचाट पारित हो जाये, अथवा
(ii) जब माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई आदेश दिया जाये।
यह एक सामान्य बात है कि जिस विवाद के लिए मामला माध्यस्थम् को सन्दर्भित किया जाता है और माध्यस्थ द्वारा उसका निपटारा कर पंचाट (Award) अन्तिम रूप से पारित कर दिया जाता है, वहाँ माध्यस्थम् कार्यवाहियों को समाप्त हो जाना स्वाभाविक है।
माध्यस्थम् कार्यवाहियों का समापन उप धारा (2) में वर्णित अवस्थाओं में भी हो जाता है।
(2) दावाकर्ता द्वारा दावे का प्रत्याहरण कर लिये जाने पर:
दावाकर्ता द्वारा दावे का प्रत्याहरण कर लेने पर भी माध्यस्थम् कार्यवाहियों का समापन हो जाता है। लेकिन इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं-
(i) प्रत्यर्थी द्वारा आदेश पर आपत्ति नहीं की जाये; तथा
(ii) माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा विवाद के अन्तिम हल को प्राप्त करने में अपनी ओर से वैध हितों को मान्यता प्रदान नहीं की जाये।
आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दावाकर्ता द्वारा दावे को वापस लेने पर माध्यस्थम् कार्यवाहियाँ समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में माध्यस्थ के लिए आगे कोई कार्यवाही करने के लिए कुछ नहीं बचता है।
(3) पक्षकारों के करार द्वारा :
विवाद के पक्षकार आपसी करार द्वारा भी माध्यस्थम् कार्यवाहियों को समाप्त कर सकते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि पक्षकार परस्पर सहमति द्वारा भी माध्यस्थम् कार्यवाहियों को समाप्त कर सकते हैं।
इस अवस्था में किसी भी पक्षकार को माध्यस्थम् कार्यवाहियों के समापन पर आपत्ति नहीं होती है। अधिकरण द्वारा वैध हितों को मान्यता देनें का प्रश्न भी नहीं उठता है।
केस – टी. श्रीनिवास राव बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर. 2009 एन.ओ.सी. 1428 आंध्रप्रदेश):
इस मामले में न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि, पक्षकार करार में मध्यस्थ की नियुक्ति को समाप्त करने का उपबन्ध कर सकते हैं और ऐसा करार प्रभावी होगा। ऐसे मामलों में मध्यस्थ की नियुक्ति को समाप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
(4) कार्यवाहियों को जारी रखना अनावश्यक या असम्भव हो जाने पर:
जहाँ माध्यस्थम् अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि माध्यस्थम् कार्यवाहियों को चालू रखना, अनावश्यक या असम्भव है, वहाँ माध्यस्थम् कार्यवाहियाँ समाप्त कर दी जाती है।
ऐसा सामान्यतः तब होता है जब पक्षकारों के बीच समझौता हो जाये या पक्षकार स्वयं ऐसी कार्यवाहियों को निरन्तर रखने में रुचि नहीं रखे।
(5) समापन की अन्य परिस्थितियाँ :
अधिनियम की धारा 32 में वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें माध्यस्थम् कार्यवाहियाँ समाप्त हो जाती हैं। यह परिस्थितियाँ निम्नांकित हैं-
(i) जब दावेदार अधिनियम की धारा 23 (1) के अन्तर्गत अपने दावे का कथन (Statement of Claim) संसूचित करने में असफल रहता है। (धारा 25)
(ii) जब विवाद समझौता पंचाट द्वारा समाप्त हो जाता है। [धारा 30(2)]
(iii) जब विवाद के पक्षकारों द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को विवाद समाप्त करने का अनुरोध किया जाता है और माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है।
(iv) जब किसी पक्षकार द्वारा मध्यिस्थम् अधिकरण की अधिकारिता (jurisdiction) को चुनौती दी जाती है और माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा ऐसी चुनौती को स्वीकार कर लिया जाता है, तब माध्यस्थम् कार्यवाहियाँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं।
(v) जहाँ धारा 38(2) के परन्तुक के अन्तर्गत एक पक्षकार निक्षेप के अपने अंश का भुगतान करने में असफल रहता है, वहाँ दूसरा पक्षकार ऐसे अंश का संदाय कर सकता है।
लेकिन जहाँ दूसरा पक्षकार भी दावे या प्रतिदावे के सम्बन्ध में पूर्वोक्त अंश का संदाय नहीं करता है, वहाँ माध्यस्थम् अधिकरण ऐसे दावे या प्रतिद। वे के सम्बन्ध में माध्यस्थम् कार्यवाहियों को निलम्बित या समाप्त कर सकेगा।
माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 32 के उपबन्ध आदर्श विधि के अनुच्छेद 32 पर आधारित हैं।
अनुच्छेद 32 का मूल पाठ इस प्रकार है-
(1) माध्यस्थम् कार्यवाही अन्तिम पंचाट द्वारा या पक्षकारों के करार द्वारा या इस अनुच्छेद के पैरा
(2) के अन्तर्गत माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश द्वारा समाप्त होती है।
(2) माध्यस्थम् अधिकरण-
(क) माध्यस्थम् कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश तब देगा जब दावेदार अपना दावा वापस ले लेता है, जब तक कि प्रत्यर्थी उस पर आपत्ति नहीं करता तथा उसकी ओर से विवाद के अन्तिम हल प्राप्त करने के उसके वैध अधिकार को माध्यस्थ अधिकरण मान्यता नहीं देता है;
(ख) माध्यस्थम् अधिकरण समाप्ति का आदेश दे सकेगा यदि किसी कारण कार्यवाही का जारी रहना अनावश्यक या अनुचित हो जाता है।
(3) माध्यस्थम् अधिकरण का प्राधिकार अनुच्छेद 33 तथा अनुच्छेद 34 के अधीन माध्यस्थ कार्यवाहियों के समाप्त होते ही समाप्त हो जायेगी।
निष्कर्ष:
माध्यस्थम् कार्यवाही, पक्षकारों के विवाद के समाधान का एक प्रभावी और आधुनिक साधन है। इसके संचालन एंव समापन सम्बन्धी नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि, माध्यस्थम् की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायोचित हो। आज के समय में जब मुकदमों का दायरा बढ़ता जा रहा है, तब माध्यस्थम् न्याय प्राप्ति का एक त्वरित, कम खर्चीला एवं विश्वसनीय विकल्प है।
महत्वपूर्ण आलेख
भारत में सूचना का अधिकार कब लागु हुआ एंव इसके मुख्य उद्देश्य कोन-कोनसे है
राज्य विधिज्ञ परिषद् क्या है? गठन, कार्य एवं शक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी
अन्तराभिवाची वाद की संपूर्ण जानकारी: परिभाषा, वाद की अन्तर्वस्तु और प्रक्रिया