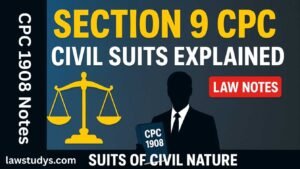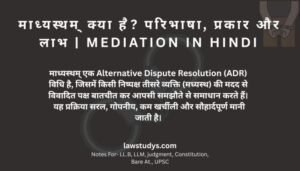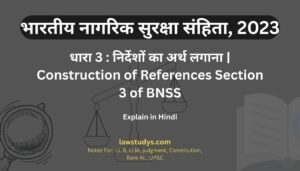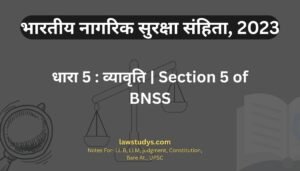सूचना के अधिकार से तात्पर्य – उस वैधानिक नागरिक अधिकार से है जो किसी देश के व्यक्ति को सरकारी कार्यकरण से सम्बन्धित सूचनाएँ प्राप्त करने के अवसर एवं पहुँच प्रदान करता है।
भारत में सूचना के अधिकार की माँग 70 के दशक में उस समय उठने लगी थी जब दिल्ली में चर्चित चोपड़ा हत्याकांड के बाद हिन्दुस्तान टाइम्स के पत्रकार ने खतरनाक अपराधियों रंगा बिल्ला से जेल में साक्षात्कार हेतु जेल प्रशासन से इस आधार पर अनुमति माँगी थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना की प्राप्ति समाहित है।
इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक आवश्यक अंग माना गया।
एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1982, एस. सी.149) –
इस मामले में सन् 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि, यदि एक समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण मनोयोग के साथ स्वीकार करता है तो वहाँ के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। इसमें न्यायालय का यह भी मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 17(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना जानने एवं प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी समाहित है।
यह भी जाने – अभिवचन किसे कहते है, इसके प्रकार एंव मुख्य उद्देश्य बताइये | लॉ नोट्स
सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ –
भारत में सूचना के अधिकार की लड़ाई मुख्य तौर पर ग्रामीण तथा निर्धन वर्ग के लोगों द्वारा लड़ी गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर 25 जुलाई 2000 को अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार ने स्वतंत्रता विधेयक 2000 प्रस्तुत किया जिसे गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने एक वर्ष पश्चात् इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के रूप में लागू हुआ।
इस अधिनियम में कमियों के कारण पुनः 23 दिसम्बर 2004 को नया सूचना का अधिकार विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। जिस पर लम्बी बहस के बाद इसे 146 संशोधनों के साथ 11 मई 2005 को लोकसभा ने इसे स्वीकार किया और अगले दिन ही इसे राज्यसभा द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया।
उसके पश्चात यह अधिनियम सन 2005 दिनांक 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया जो कुल 31 धारायें तथा दो अनुसूचियों में विभक्त है।
देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जम्मू-कश्मीर कैडर के पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी वजाहत हबीबुल्ला को बनाया गया जिसे 26 अक्टूबर 2005 को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा शपथ दिलवायी गई।
यह भी जाने – साक्ष्य कानून में सह अपराधी कौन है? साक्ष्य में उसकी स्थिति और कथन का क्या महत्त्व है?
सूचना के अधिकार में शामिल अधिकार
(i) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण
(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना
(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने देना
(iv) डिस्केट फ्लापी, टेप वीडियो कैसेट के रूप में सूचना अभिप्राप्त करना आदि।
मुख्य उद्देश्य
(i) लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाना तथा उसके उत्तरदायित्व में संवर्धन करना।
(ii) लोक प्राधिकारियों के नियंत्रधीन सूचना तक जनसाधारण की पहुँच सुनिश्चित करना।
(iii) भ्रष्टाचार को रोकना।
(iv) केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करना।
(v) सरकारों के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।