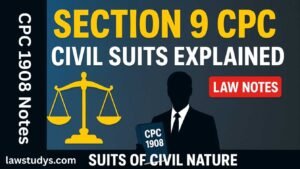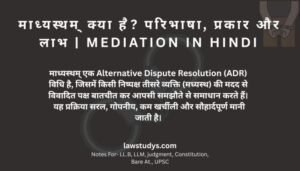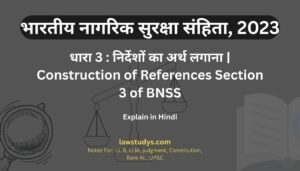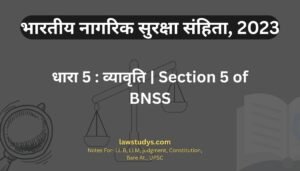इस लेख में बाल अपराध (किशोर अपराध) के बारे में बताया गया है | कानून में बाल अपराधी कोन होता है और बाल अपराधी के कारण तथा इसको कैसे रोका जा सकता है? और बाल अपराधियों को सुधारने के लिए क्या उपाय किये जा सकते है, पर संक्षेप में चर्चा की गई है,
यदि आप वकील, विधि के छात्र या न्यायिक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे है, तब आपके लिए बाल अपराधी एंव उसके बारें में जानना बेहद जरुरी है –
परिचय – बाल अपराध क्या है
वर्तमान समय में बाल अपराध समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है जो निरंतर फैल रही है| बाल अपराध को बच्चों के साथ होने वाले अपराध के रूप में जाना जाता है, जिससे समाज एक बड़ा वर्ग प्रभावित है।
बाल अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो बच्चों के साथ होते हैं और उनके भविष्य के साथ साथ वर्तमान को प्रभावित करते है, जिस कारण बच्चो को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है।
आसान शब्दों में जब किसी बच्चे द्वारा कानून या समाज के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है, तब उसे बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है जिसे किशोर अपराध अथवा बाल अपचारिता (Juvenile delinquency) भी कहा जाता है|
किशोर न्याय कानूनों में अपराध शब्द की जगह अपचारिता शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि समाज का मानना है कि बच्चे कभी अपराध नहीं करते, उनके कृत्य अभद्र, अशिष्ट या निन्दनीय हो सकते हैं, लेकिन वे कभी दण्ड योग्य नहीं हो सकते।
भारत में बाल न्याय अधिनियम, 1986 (संशोधित 2000) के तहत 16 वर्ष की आयु तक के बालकों एंव 18 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं द्वारा किये गए कानून विरोधी कार्य बाल अपराधी की श्रेणी में आते है| यह अलग बात है की राज्य एंव देश के अनुसार बाल अपराधी की अधिकतम आयु सीमा भी अलग हो सकती है|
बाल अपराध के सम्बन्ध में हम केवल आयु को ही निर्धारित नहीं मान सकते इसमें कभी कभी अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानि 7 से 16 का बालक या 7 से 18 वर्ष की बालिका द्वारा कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसकी सजा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास है, उस स्थिति में हम उन्हें बाल अपराधी नहीं मान सकते, जैसे – हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि कार्य को करना|
यह भी जाने – अपराध से आप क्या समझते हैं? | परिभाषा, प्रकार एवं चरण (Concept Of Crime In Hindi)
बाल अपराध की परिभाषा
बाल अपराध (बाल अपचारिता) की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है जबकि अनेक अपराधशास्त्रियों ने इसकी अपने-अपने ढंग से परिभाषायें दी है, जिनमे मुख्य परिभाषायें निम्न है –
डॉ. एम. जे. सेठना के अनुसार – बाल अपराध के अन्तर्गत किसी ऐसे बच्चे अथवा किशोर व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो तत्समय प्रचलित विधि द्वारा निर्धारित आयु के भीतर है।
डॉ. पी. एन. वर्मा के अनुसार – बाल अपचारिता से तात्पर्य कर्त्तव्यो की उपेक्षा अथवा उल्लंघन से है, एक गलती से है।
रॉबिन्सन के अनुसार – बाल अपराध से तात्पर्य आवारागर्दी, भिक्षावृत्ति, शैतानी, दुर्व्यवहार, उद्दण्डता आदि प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों से है।
सिद्धिकी के मतानुसार – विधि द्वारा विनिर्दिष्ट आयु तक के बालकों के लिए निषेधित कार्य का किया जाना बाल अपराध है और जो बालक इस प्रकार बाल अपराध करता पकड़ा जाये, वह बाल अपराधी अर्थात् अपचारी बालक कहलाता है।
काल्डनेल के शब्दों में – अपचारिता से तात्पर्य किशोरों द्वारा किये जाने वाले ऐसे कृत्यों से है जो राज्य के संरक्षणाधीन आ जाते हैं।
इसी तरह न्यू मैक्सिको विधि के अनुसार – बाल अपराधी वह बालक है जो अपने माता-पिता अथवा संरक्षक के विधिपूर्ण आदेशों की जानबूझकर निरन्तर अवहेलना करने के कारण आदतन अनियंत्रित, अवज्ञाकारी अथवा हठधर्मी समझा जाता है अथवा जो घर या विद्यालय से आदतन भगोडा है या जो आदतन अपनी या दूसरों की नैतिकता, स्वास्थ्य एवं कल्याण को क्षति कारित करने वाले या संकट में डालने वाला आचरण करता है।
यह भी जाने – भारत में सूचना का अधिकार का इतिहास, उद्देश्य एंव महत्त्व (History of Right to Information in India)
रुबिन ने बाल अपराध के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों को शामिल किया है जिनमे से कोई कार्य बच्चो द्वारा किया जाता है तो उन्हें बाल अपराधी माना जाएगा, ऐसे कृत्य निम्नलिखित है –
(क) किसी विधि नियम अथवा अध्यादेश की अवज्ञा करना,
(ख) अनैतिक एवं अश्लील आचरण करना,
(ग) चरित्रहीन एवं अनैतिक लोगों की संगति,
(घ) कुख्यात स्थानों में विचरण करना,
(ड) वेश्यालयों एवं जुआघरों में संरक्षण,
(च) मदिरालयों में संरक्षण,
(छ) अनावश्यक रात्रि में सड़कों व गलियों में भ्रमण करना
(ज) अनाधिकृत रूप से रेल, बस या इंजिन आदि पर चढ़ना;
(झ) घर अथवा विद्यालय से निरन्तर गायब रहना,
(ञ) सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील भाषा का प्रयोग करना अथवा आचरण करना,
(ट) गलियों में सोना या मटरगस्ती करना,
(ठ) भिक्षा माँगना, धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन करना,
(ड) अवैध व्यवसाय करना आदि।
यहाँ यह बताना उचित होगा कि, अधिनियम में बाल अपराधी जैसा कोई शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया है, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में शब्द अपचारी किशोर प्रयुक्त किया गया था और वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में भी शब्द बाल अपराधी का उपयोग ना करके विधि विवादित किशोर का प्रयोग किया गया है।
यह भी जाने – सीपीसी के तहत डिक्री के निष्पादन के विभिन्न तरीके क्या है | Mode Of Execution Order 21 Rule 26 To 36 CPC
बाल अपराध के कारण
सम्पूर्ण मानव सभ्यता में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमे अपराध घटित नहीं होते है और उन अपराधो बाल अपराध एक प्रमुख समस्या है क्योंकि जब मानव बचपन से ही अपराध की दुनिया में शामिल हो जाता है तब उसके सुधरने एंव समाज में योगदान की संभावना नहीं होकर समय के साथ साथ उसके अपराध में बढ़ोतरी होने की संभावना बन जाती है|
यहाँ हमारे लिए यह जानना जरुरी है की बालक अपराध क्यों करता है और उसके अपराध कारित करने में कोनसे तत्व उत्तरदायी है, इस सम्बन्ध में अपराधशास्त्रियों ने बाल अपराध के एक नहीं, बल्कि अनेक कारण बताये है जिन पर आज भी अनुसंधान जारी है, जो निम्न है –
(i) पारिवारिक वातावरण
बाल अपराधों का पहला कारण पारिवारिक वातावरण को माना जाता है। परिवार मे बालक को जैसा वातावरण मिलता है. बालक वैसा ही बन जाता है। यदि परिवार में बालक को अच्छा वातावरण मिलता है तो बालक का व्यवहार भी अच्छा बन जाता है जबकि इसके विपरीत वातावरण मिलने पर वह अपराधी बन बैठता है, इसी कारण परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला माना गया है।
विघटित परिवार के बालकों को अक्सर आपराधिक प्रवृत्ति का माना जाता हैं यानि ऐसे परिवार जिसमें माता-पिता या संरक्षक नहीं हो या माता-पिता के मध्य विवाह विच्छेद हो गया हो या पति-पत्नी दोनों अलग-अलग रह रहे हो या पिता घर से अधिक समय तक दूर रहत है, वहां पर बालक अनुशासनहीन बन जाते हैं, क्योंकि उन पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं होता।
इसी तरह परिवार का ‘अनैतिक वातावरण’ भी बालक को अपराधी बनाने में योगदायी होता है, ऐसे परिवार जिसमे भाई-बहिन अपराधी है या परिवार के सदस्य आपस में लड़ते रहते है या परिवार में माता-पिता अथवा सौतेले माता-पिता द्वारा बच्चो का तिरस्कार किया जाता है, या परिवार में वेश्यावृत्ति, जुआ, मदिरापान आदि होता है तो बच्चों पर इनका कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
इसके अलावा सन्तान का अवैध होना, सन्तान के साथ सौतेला व्यवहार करना, मारपीट करना भीड भरे स्थानों में रहना आदि भी बाल अपराध के कारण बनते हैं।
यह भी जाने – अपराध के तत्व क्या है जो एक अपराध का गठन करते है | Elements Of Crime in Hindi
(ii) निर्धनता
बाल अपराध का दूसरा बड़ा कारण अर्थाभाव यानि निर्धनता है। जब परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तब बालकों का भरण-पोषण, शिक्षा-दीक्षा तथा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और इसके परिणामस्वरूप बालक चोरी, भिक्षावृत्ति अथवा यौन अपराध के शिकार हो जाते हैं।
कुप्पूस्वामी (kuppuswamy, P. 423) के अनुसार – बच्चे में अपराधी चरित्र का विकास करने में निर्धनता एक महत्वपूर्ण कारक है| इसी गरीबी के कारण कई बार बच्चों में हीन भावना भी जन्म लेने लगती है और इसी हीन भावना के कारण वे अपराध की ओर जाने लगते हैं।
(iii) उपेक्षा
परिवार में बालकों की उपेक्षा भी बाल अपराध का एक अहम कारण है। जब बालको को माता-पिता का नैसर्गिक स्नेह नहीं मिलता है तो उनमें कुण्ठायें पैदा हो जाती हैं और वे उद्दण्ड एवं अनुशासनहीन बन जाते हैं। माता-पिता के स्नेह के अभाव में बालकों में आत्मविश्वास भी पैदा नहीं हो पाता और इसकी उपेक्षा के चलते बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती जिससे वे अपराधिक प्रवृत्तियों को अपनाने लगते हैं।
(iv) शारीरिक कारण
जब बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग, कुरूप, नेत्रहीन आदि होता है तब समाज में उसे उपहास का पात्र समझा जाता है तथा ऐसे बच्चों में हीन भावना भी पनपने लगती है। ऐसे बच्चों को न तो रोजगार मिल पाता है एंव न ही उनका विवाह हो पाता है और उनके आत्म-सम्मान को ठेस भी पहुंचती है। इसके फलस्वरूप वे अपने उपहास का बदला लेने के लिए दूसरो को नुकसान पहुंचाने लगते है और ऐसी स्थिति में वे अपराधी बन जाते हैं।
(v) मानसिक विकृतता
मानसिक तौर पर बालक का विकृत होना भी बाल अपराध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। मानसिक विकृतता के कारण बालको में अपना हित-अहित सोचने की क्षमता नहीं होती और न वे अच्छे-बुरे के बीच अन्तर कर पाते हैं। उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे बालक चोरी, भिक्षावृत्ति, यौन-सम्बन्ध जैसे आपराधिक कृत्यों की ओर उन्मुख हो जाते हैं।
(vi) अश्लील साहित्य
साहित्य का व्यक्ति एवं व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव पडता है। व्यक्ति जैसा साहित्य पढ़ता है उसका मन व आचरण वैसा ही बन जाता है। अच्छे साहित्य से “व्यक्ति सुसंस्कारित बनता है तो अश्लील साहित्य से अपराधी यौन साहित्य, जासूसी उपन्यास कॉमिक्स, जैसे साहित्य को पढ़कर बालक चोरी, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति जैसे अपराध कारित करने लगते हैं”।
इसके अलावा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कामोत्तेजक लेख-आलेख, अश्लील चित्रों, सेक्सी कहानी-किस्सो आदि से बच्चों का मन विकृत होकर अपराधी बन जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साहित्य वरदान भी है और अभिशाप भी।
(vii) सिनेमा, दूरदर्शन एवं इन्टरनेट
सिनेमा, दूरदर्शन एवं इन्टरनेट भी बाल अपराधों के लिए उत्तरदायी है। सिनेमा हॉल में एवं दूरदर्शन पर कई बार अश्लील चित्र एवं फिल्में दिखाई जाती हैं जिनसे निर्दोष बच्चे भी दोषी बन बैठते है। ऐसी फिल्मों एवं चित्रों का बच्चों के चरित्र पर कुप्रभाव पड़ता है तथा वे अपराधी बन बैठते हैं।
इस तरह के अनेक मामले हमारे सामने आते रहते है, जैसे – दिल्ली (भारत) के विद्यालय का एक छात्र इन्टरनेट पर लड़कियों के अश्लील चित्र बनाते पकड़ा गया था तब उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की गई थी।
(viii) संगति
संगति का भी बालक पर काफी प्रभाव पड़ता है। बालक जैसी संगति में रहता है, वह वैसा ही बन जाता है। यदि बालक कुख्यात अपराधियों की संगति में रहता है तो वह भी अपराधी बन जाता है। यही कारण है कि बालक अपराधियों के लिए सुधारात्मक दण्ड की व्यवस्था की गई है ताकि वे कारागृहों में कुख्यात अपराधियों की संगति से बच सके।
बच्चों को सुधारने के दृष्टि से माननीय न्यायालय ने अपने अनेक मामलों में बाल अपराधियों को कारागृहों में कुख्यात अपराधियों की संगति से बचाने के लिए ही उन्हें जमानत पर छोड़ दिये जाने की अनुशंसा भी की है।
(ix) राजनीतिक संरक्षण
बाल अपराधों में अभिवृद्धि का एक प्रमुख कारण राजनीतिक संरक्षण एवं स्वार्थ सिद्धि को भी माना जाता है। राजनेता अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए विद्यालय के बच्चों का खुलकर प्रयोग करते हैं। विद्यालयों में हड़ताल, तोड़फोड, घेराव, हिंसा आदि अधिकांश राजनेताओं के इशारों पर ही होती है।
चुनावों में बालशक्ति (युवाशक्ति) का खुलकर दुरुपयोग किया जाता है जिससे ऐसी प्रवृतियों में लिप्त रहते हुए बालक एक दिन अपराधी बन जाता है।
(x) बाल विवाह
बाल विवाह को भी बाल अपराधों का कारण माना गया है। कम आयु में विवाह हो जाने से बालक या बालिका अपने दाम्पत्य कर्तव्यों से अनजान रहते हैं और वे आगे जाकर लैंगिक अपराधों के शिकार हो जाते हैं या लैंगिक अपराध कर बैठते हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति दायित्व बोध नहीं होता।
इस कारण वर्तमान समय में बाल विवाह को माननीय न्यायालय द्वारा शून्यकरणीय (Voidable) घोषित कर दिया गया है। (टी. शिवकुमार बनाम इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस, ए.आई.आर. 2012 मद्रास 62)
बाल अपराध को कैसे रोका जा सकता है
जैसा की हम जानते है की बाल अपराध समाज के एक खतरा है जो बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है, ऐसी स्थिति में बाल अपराधों की रोकथाम के अनेक उपायों पर भी विचार किया गया जिनके द्वारा बाल अपराधों पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है –
(i) पारिवारिक स्नेह
जिस तरह बाल अपराधों का पहला कारण पारिवारिक वातावरण है उसी तरह उनके निवारण का प्रथम दायित्व भी परिवार पर अर्थात् माता-पिता पर ही है। माता-पिता एवं परिजनों को चाहिये कि वे अपने बच्चों को नैसर्गिक स्नेह प्रदान करें, उनके साथ कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं करें, मारपीट एवं गाली गलौच नहीं करें|
इसके अलावा परिवारजन को चाहिए की वे अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दें, अपने परिवार को विघटन से बचायें, परिवार में अनैतिक वातावरण नहीं पनपने दें और माता-पिता अत्यधिक भीड़ भरे स्थानों में परिवार सहित रहने से बचे, आदि बातों का पालन करके बच्चों को बाल अपराधी बनाने से रोका जा सकता है।
(ii) आर्थिक स्थिति
बाल अपराधों के निवारण के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना आवश्यक है। परिवार के वयस्क व्यक्ति रोजगार में लगे रहें, कर्ज से बचें, घरेलू उद्योग-धन्धों में अभिवृद्धि करें, श्रम से जी नहीं चुरायें, अनावश्यक व्यय से बचें तो बाल अपराधों में कमी आ सकती है।
जब परिवार में आर्थिक स्थिति सुदृढ होगी तो बच्चों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी, परिवार में अनैतिक वातावरण नहीं पनपेगा, हीन भावना जन्म नहीं लेगी और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा।
(iii) समुचित शिक्षा
बच्चों को समुचित शिक्षा दिया जाना भी अपेक्षित है। सर्वप्रथम तो बालकों को विद्यालयों में भेजा जाये, उन्हें अशिक्षित नहीं रहने दिया जाये, चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाये, उन्हें सुसंस्कारित बनाया जाये तथा धर्म के प्रति आस्था की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया जाये।
(iv) स्वस्थ मनोरंजन
बालाकों के लिए स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था की जाये। उन्हें चरित्र निर्माण एवं आदर्श की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित करने वाले चलचित्र दिखाये जाये. बस्तियों व मोहल्लों में बाल उद्यान लगाये जाये तथा मनोरजन के साधन जुटाये जाये। बालको को अश्लील चलचित्रों, सिनेमा गृहों एवं सैक्सी चालों से दूर रखा जाना भी अपेक्षित है।
(v) सद् साहित्य
बालकों के लिए सद् साहित्य जुटाया जाये। उन्हें अश्लील साहित्य से दूर रखा जाये। जासूरी उपन्यास, कॉमिक्स आदि उनके हाथ में न आने दें। महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग, धार्मिक पुस्तकें, चरित्र निर्माण की साहित्य सामग्री तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जाये। इसके लिए गाँव-गाँव में अच्छे पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किये जा सकते हैं।
(vi) पुनर्वास
उपेक्षित एवं भगोड़े बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था किया जाना भी आवश्यक है। बच्चों को सुधारग्रहों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं काम दिया जाये, उनके लिए रोजगार के अवसर तलाशे जायें। जब बालक रोजगार में लगा रहेगा तो उसे अपराधों की ओर जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा।
(vii) सुधार गृहों की स्थापना
अपचारी बालकों में सुधार लाने के लिए सुधार गृहों की स्थापना किय जाना भी अपेक्षित है ताकि वहाँ बालकों की शिक्षा-दीक्षा, भोजन, आवास चिकित्सा आदि की व्यवस्था समुचित रूप से हो सके। यह सुखद है कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 में अपचारी बालकों के लिए सप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बालक गृह, आश्रय गृह, धातृ देखरेख, पश्चात्वर्ती देखरेख आदि की व्यवस्था की गई है।
(viii) राजनीतिक प्रदूषण
बच्चों को राजनीतिक प्रदूषण से बचाया जाना आवश्यक है। राजनेता अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बच्चों को प्रयोग नहीं करें, उनका चुनावों में उपयोग नहीं करें एंव ना ही उन्हें विद्यालयों में हडताल, हिंसा, बन्द, घेराव, तोड़फोड आदि के लिए दुष्प्रेरित नहीं करें।
(ix) पृथक न्यायिक व्यवस्था
बाल अपराधियों (अपचारी किशोरों) से सम्बन्धित मामलों के लिए पृथक न्यायिक व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत –
(क) पृथक बाल न्यायालय स्थापित किये जायें,
(ख) त्वरित विचारण किया जाये,
(ग) जमानत की उदार-व्यवस्था हो,
(घ) दण्ड के स्थान पर सुधार के अवसर प्रदान किये जायें, तथा
(ङ) परिवीक्षा, भर्त्सना पैरोल आदि की समुचित व्यवस्था की जाये।
(x) मनोवैज्ञानिक चिकित्सा
अपचारी बच्चों को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा दी जाये। बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञों तथा मनोचिकित्सकों से ऐसे बालकों का परीक्षण कराया जाये तथा उनके लिए सुधार के उपाय सुझाये जायें।
इस प्रकार के उपाय करके बाल अपराधियों को सुधारा भी जा सकता है और बाल अपराधों का निवारण भी किया जा सकता है।
सम्बंधित पोस्ट –
नोट – पोस्ट से सम्बंधित सामग्री एंव अपडेट जरुर शेयर करें।
संदर्भ – किशोर न्याय विकिपीडिया