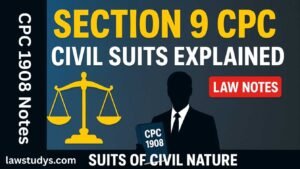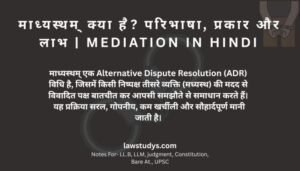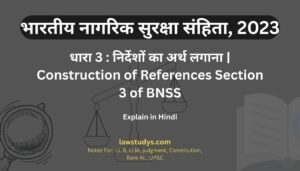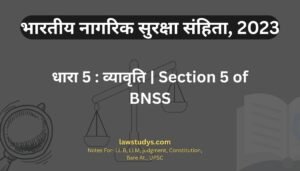इस लेख में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है, यह रिपोर्ट कौन दर्ज करा सकता है? तथा इसका महत्त्व एंव दर्ज करवाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए | एफआईआर क्या है? FIR कब और कैसे दर्ज की जाती है के बारे में बताया गया है,
यदि आप वकील, विधि के छात्र या न्यायिक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे है, तो ऐसे में आपको FIR (फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) के बारे में जानना बेहद जरुरी है –
प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर ) क्या होती है?
प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है। यह उस सूचना की रिपोर्ट होती है जो किसी अपराध के घटने पर सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है इसलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।
पुलिस सिर्फ संज्ञेय अपराध के मामलों में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है। संज्ञेय अपराध ऐसे गंभीर अपराध को कहा जाता है जिसमें पुलिस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच भी शुरू कर सकती है। यह दिगर है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध को संज्ञेय बताया गया है तो पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अवश्य रूप से दर्ज करनी चाहिए।
यह भी जाने – समन की तामील क्या है, प्रतिवादी पर समन जारी करने के विभिन्न तरीके
प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को शुरू करती है। प्रक्रियात्मक कानून के अनुसार थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर सकती है और यदि मामला अदालत तक पहुंचता है तो ट्रायल के दौरान एफआईआर की जांच की जाती है ।
इसलिए यह अनिवार्य है कि शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी में जितने भी घटना से सम्बंधित तथ्य है उन सभी को एफआईआर में दर्ज किया जाना चाहिए ।
यह एक सुस्थापित कानून है कि जब भी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रथम सूचना प्राप्त होती है तब एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य हो जाती है। पुलिस ऐसा कभी नहीं कह सकती है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले प्रथम सूचना को सत्यापित करने के लिए प्राथमिक जांच करें (उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ विशेष अपराध को छोड़कर)|
पुलिस प्राथमिक जांच तभी कर सकती है जब प्रथम सूचना के आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि, किया गया अपराध संज्ञेय है अथवा गैर-संज्ञेय| यानि संज्ञेय अथवा गैर-संज्ञेय अपराध प्रत्येक मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है।
प्राथमिकी का उद्देश्य सिर्फ यह निर्धारित करना है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है या नहीं, ना कि प्राप्त सूचना को सत्यापित करना है।
उच्चतम न्यायालय के निर्णय, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य में यह कहा गया है कि, जांच सात दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए|
यह भी जाने – न्यायालय कब अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है | आदेश 39 के तहत प्रावधान
प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन दर्ज करा सकता है?
अपराध का पीड़ित व्यक्ति या अपराध का साक्षी या कोई भी व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानता है वह पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है, इसके अलावा कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है स्वयं ही एफआईआर दर्ज करा सकता है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में निर्धारित है| प्रत्येक बार एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस को इस प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है। एफआईआर पुलिस को लिखित में या मौखिक रूप में दी जा सकती है। जैसे –
– यदि आप मौखिक रूप से सूचना देते है तो पुलिस अधिकारी आपको सूचना को बयान करने के लिए कहेगा ताकि वह जहां तक संभव हो सके वह आपके ही शब्दों में साधारण और स्पष्ट भाषा में बयान को लिख सके,
- सूचना देने वाले या शिकायत करने वाले एक व्यक्ति के रूप में आपका यह अधिकार है कि पुलिस द्वारा रिकार्ड की गई सूचना वह आपको पढ़कर सुनाए;
- एफआईआर तैयार होते ही उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, आपको इस पर तभी हस्ताक्षर करने चाहिए जब आप सुनिश्चित हो जाए कि पुलिस द्वारा रिकार्ड की गई सूचना आपके द्वारा दी गई सूचना से मिलती है। ध्यान रहे कि एफआईआर में वह सभी जानकारी हो जो आप जानते हैं ।
- वैसे व्यक्ति जो पढ़ या लिख नहीं सकते, उन्हें एफआईआर पर तभी अपने बाएं अंगूठे का निशान देना चाहिए जब आप संतुष्ट हो जाएं कि बयान सही रिकार्ड किया गया है ।
आपका यह अधिकार है कि एफआईआर की प्रति आपको तत्काल और निःशुल्क मिले । यदि पुलिस आपको एफआईआर की प्रति नहीं देती है तो आप इसकी अवश्य मांग करें ।
- पुलिस को थाने की डायरी में एफआईआर की तारीख और विषय अवश्य दर्ज करनी चाहिए|
यह भी जाने – लोक दस्तावेज एवं प्राइवेट दस्तावेज क्या है | साक्ष्य अधिनियम धारा 74 एवं धारा 75
लिंग आधारित अपराध की शिकार महिलाएं
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) में कुछ लिंग आधारित यौन अपराधों के बारे में बताया गया है जिसके लिए एफआईआर दर्ज करने की विशेष प्रक्रिया है।
यदि पीड़ित महिला स्वयं एफआईआर दर्ज करने पुलिस थाने आती है तो उसका एफआईआर किसी महिला पुलिस अधिकारी अथवा किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाना चाहिए।
यदि पीड़ित महिला मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है (अस्थायी तौर पर भी) तो एफआईआर उसके घर पर, उसकी पसन्द के किसी स्थान पर एक भाषान्तरकार, विशेष शिक्षक की उपस्थिति में ही दर्ज की जानी चाहिए तथा इसका वीडियो भी तैयार किया जाना चाहिए।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) के अंतर्गत बताए अपराधों पर एफआईआर दर्ज करने से इंकार करना किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए एक दंडनीय अपराध होगा ।
यदि कोई पुलिस अधिकारी इनमें से किसी भी अपराध पर एफआईआर दर्ज करने में असफल होता है तो वह छह महीने की अवधि के कारावास के दंड का हकदार होगा जिसे दो वर्ष की अवधि तक भी बढ़ाया जा सकता है, तथा उसे जुर्माना भी देना होगा । ( भारतीय दंड संहिता की धारा 166क (ग))
यह भी जाने – सुने जाने के अधिकार का सिद्धांत | महत्त्व एंव आवश्यक तत्व | Locus Standi in hindi
शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट
यदि सूचित किया हुआ अपराध किसी थाने के क्षेत्राधिकार के बाहर होता है तब भी कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकता है। जहाँ कोई अपराध किसी थाने के क्षेत्राधिकार से बाहर घटित होता है तथा उस थाने में उस अपराध की एफआईआर दर्ज की जाती है तब उसे शून्य एफआईआर कहा जाता हैं|
शून्य एफआईआर दर्ज करने,के बाद उसकी रजिस्टर में प्रविष्टी करने और संबंधित थाने को उसे भेजने को वह थाना बाध्य है। इसके अलावा पुलिस पीड़ित पक्षकार को यह भी बताएगी कि उसने किस थाने को एफआईआर भेजी है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या शामिल करना चाहिए
– पीड़ित पक्ष या सूचना देने वाले को अपना नाम व पता;
– उस घटना की तारीख, समय और स्थान जिसकी सूचना दी जा रही हैं;
– घटना जैसे घटी है उसका सही-सही तथ्य और साथ ही अपराध के घटित होने के तरीके का ब्यौरा।
उदाहरण के लिए –
– शरीर पर लगे घाव या इस्तेमाल किए गए हथियार, घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और विवरण आदि।
– यदि अभियुक्त का नाम नहीं मालूम हैं तो उसकी पहचान करने में सहायक कोई विवरण जैसे कि आयु, लिंग, शरीर का गठन, लम्बाई या पहचान की कोई विशेषता या उसके शरीर का कोई निशान या उसकी आवाज,
– गवाहों के नाम और ब्यौरा यदि कोई हो ।
पीड़ित पक्ष या सूचना देने वाले को क्या नहीं करना चाहिए?
– गलत शिकायत नहीं दर्ज करवानी चाहिए और ना ही पुलिस को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए।
– गलत जानकारी देने या पुलिस को गुमराह करने पर कानून के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है ( भारतीय दंड संहिता धारा 203);
– तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर या तोड़-मरोड़कर नहीं बताना चाहिए
– अस्पष्ट भाषा एंव वक्तव्य न दें
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर क्या करें
– पीड़ित पक्ष या सूचना देने वाला पुलिस अधीक्षक (एसपी) या पुलिस उप-महानिरीक्षक और पुलिस महा – निरीक्षक जैसे उच्च अधिकारियों से मिलकर उनका ध्यान में अपनी शिकायत ला सकता है,
– संबंधित पुलिस अधीक्षक को अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं या डाक से भेज सकते हैं। यदि एसपी आपकी शिकायत से संतुष्ट है तो वह मामले की जांच स्वयं कर सकते हैं या जांच करने का आदेश भी दे सकते हैं,
– इसके बाद भी यदि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तब उस घटना से सम्बंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत में संबंधित मैजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करवा सकते हैं,
– यदि पुलिस कानून लागू नहीं करती या इसे पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट तरीके से लागू करती है तो आप राज्य मानवाधिकार आयोग को शिकायत कर सकते हैं। यदि आपके राज्य में आयोग नहीं है तो पीड़ित पक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता हैं ।
– यदि आपके राज्य में पुलिस शिकायत प्राधिकरण है तो उसे शिकायत कर सकते हैं । ये राज्य के विशेष निकाय होते हैं जो पुलिस के खिलाफ नागरिक की शिकायत की जांच करते हैं:
– यदि पीड़ित पक्ष महिला है और यौन अपराध से पीड़ित है तब वह भारतीय दंड संहिता की धारा 166क (ग) के अंतर्गत संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती हैं।
यहाँ यह जानना जरुरी है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस जांच नहीं करने का निर्णय ले सकती है, यदि पुलिस अधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि,
(i) मामला गंभीर स्वरूप का नहीं है, या
(ii) जांच करने के पर्याप्त आधार नहीं है।
तथापि पुलिस की जांच न करने के कारण को रिकार्ड करना चाहिए और आपको तत्काल सूचना देनी चाहिए कि जांच नहीं किया जाएगा । (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 157)
महत्वपूर्ण आलेख
What is Public Interest Litigation? and its importance in India
What is the Schools of Criminology And how many Types are there? – Criminology
सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रकृति एंव उद्देश्य | Nature and purpose of the CPC
अपराधशास्त्र की परिभाषा, अर्थ एंव अपराधशास्त्र का महत्त्व | Criminology in Hindi
भारत में विधि के स्रोत : अर्थ एंव इसके प्रकार | विधि के औपचारिक और भौतिक स्रोत क्या हैं?
नोट :- इस लेख को तैयार करने में सावधानी बरती गई है लेकिन फिर भी हमारी वेबसाइट lawstudys.com किसी भी प्रकार की त्रुटि या व्याकरणिक एवं भाषाई अशुद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।