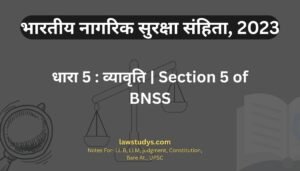प्रत्यायोजित विधायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विधायिका अपनी विधायी शक्तियों (जैसे नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश) को बनाने के लिए कार्यपालिका या स्थानीय निकाय को सौंपती है। भारत में इसका विकास एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें कई तत्वों का योगदान है।
इस लेख में प्रत्यायोजित विधायन किसे कहते है, परिभाषा एंव इसकी सीमाएं और भारत में प्रत्यायोजित विधायन के विकास मेंसहयोगी तत्वों को आसान शब्दों में बताया गया है-
प्रत्यायोजित विधायन
प्रत्यायोजित विधायन, विधि निर्माण की महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। वस्तुतः विधि-निर्माण का मुख्य रूप से कार्य विधायिका का है। विधि-निर्माण के इस कार्य को सिद्धान्ततः किसी अन्य निकाय या व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता।
लेकिन जब से लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है, तब से विधायिका के विधि-निर्माण के कार्य में आशातीत अभिवृद्धि हुई है।
वर्तमान में विधायिका के पास इतना समय नहीं है कि, वह स्वयं ही सभी विधियों, उप विधियों, नियमों, विनियमों आदि का निर्माण कर लेवें।
इस कारण वह मोटे तौर पर सिद्धान्तों एवं नीतियों को समाहित करने वाली विधियों का ही निर्माण करती है और शेष कार्य कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ देती है, जिस कार्य को ‘प्रत्यायोजित विधायन’ कहा जाता है।
प्रत्यायोजित विधायन को Subordinate Legislation, Administrative Legislation अथवा Skeleton Legislation भी कहा जाता है।
प्रो. वेड एवं फिलिप्स के अनुसार – वर्तमान काल में प्रशासन के विस्तृत कार्यों तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में राज्य के कार्यों में अभिवृद्धि के कारण संसद के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह परिनियमित उपकरणों के निर्मित करने का कार्य मन्त्रियों को सौंप दें।
यह भी जाने – साक्ष्य कानून में सह अपराधी कौन है? साक्ष्य में उसकी स्थिति और कथन का क्या महत्त्व है?
परिभाषा | Definition
प्रत्यायोजित विधायन की एक सार्वभौम परिभाषा दिया जाना कठिन है, क्योंकि प्रत्यायोजित विधायन की परिभाषा को दो अर्थों में देखा जा सकता है – एक प्रत्यायोजन की परिभाषा के अर्थ में एवं दूसरी प्रत्यायोजित विधायन की परिभाषा के अर्थ में।
प्रत्यायोजन की परिभाषा | Definition of Delegation
किसी शक्ति को एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय को सौंपा जाना प्रत्यायोजन कहलाता है, इसमें अवशेषित शक्तियाँ अर्थात् प्रतिसंहरण एवं संशोधन की शक्तियाँ प्रत्यायोजक के पास ही सुरक्षित रहती है।
इन्दिरा नेहरू गाँधी बनाम राजनारायण (1976) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि, प्रत्यायोजन का आशय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में सन्निहित शक्तियों का दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्रयोग करने का अधिकार इस रूप में सौंपना कि प्रतिसंहरण या संशोधन करने की पूर्ण शक्तियाँ प्रत्यायोजक या अनुदाता के पास बनी रहे।
प्रत्यायोजित विधायन की परिभाषा
विधान मण्डलों द्वारा विधायी शक्तियों का कार्यकारिणी को प्रत्यायोजित किया जाना ही, प्रत्यायोजित विधायन है। आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ विवशताओं के अधीन विधायिका द्वारा विधायी कार्यों को कार्यपालिका के हाथों में सौंप देना, प्रत्यायोजित विधायन है। इसे दो अर्थों में ग्राह्य किया गया है –
(i) जब विधायिका द्वारा अपने विधायी कृत्य कार्यपालिका को सौंप दिये जाते है तब उसे प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है, एवं
(ii) जब कार्यपालिका द्वारा अपने को सौंपे गये विधि-निर्माण के कार्य के अन्तर्गत नियम, विनियम, आदेश, निदेश आदि जारी किये जाते है तब उसे भी प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है।
इस प्रकार प्रत्यायोजित विधान एक ऐसा विधान है जो विधायिका से अलग किसी अन्य निकाय द्वारा बनाया जाता है। सामान्यतः इसके अधीन सारभूत विधियों का निर्माण तो विधायिका द्वारा किया जाता है लेकिन ऐसी विधियों को क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाता है जो नियम, विनियम आदि का निर्माण करती है।
यह भी जाने – अभिवचन किसे कहते है, इसके प्रकार एंव मुख्य उद्देश्य बताइये | लॉ नोट्स
प्रत्यायोजित विधायन की सीमाएं
प्रारम्भ से ही यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या विधायिका द्वारा अपनी विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन कार्यपालिका को किया जा सकता है या इसकी कोई सीमा भी है, इस सम्बन्ध में दिल्ली लॉज एक्ट,1912 का मामला विख्यात एवं मार्गदर्शक मामला है।
इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यायोजित विधायन की सीमा के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया, जैसे –
(i) विधि-निर्माण का प्रत्यायोजन एक निर्धारित सीमा से बाहर नहीं किया जा सकता है।
(ii) आवश्यक विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है।
(iii) विधायिका द्वारा आवश्यक विधायी कृत्यों का परित्याग अथवा अभ्यर्पण (Surrender) नहीं किया जा सकता है।
(iv) आवश्यक विधायी कृत्यों में कम-से-कम विधायी नीति का अवधारण और आचरण से आबद्धकर रूप में उसकी संरचना अवश्य होनी चाहिये।
(v) प्रत्यायोजन की शक्ति विधायी शक्ति की अनुपंजिगक है।
दिल्ली लॉज एक्ट (ए.आई.आर. 1951 एस.सी. 322) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि, प्रत्यायोजन की एक सीमा है और उस सीमा से हट कर विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। यदि विधायी शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
इस सम्बन्ध में हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 554) का महत्वपूर्ण प्रकरण अवलोकन योग्य है
भारत में प्रत्यायोजित विधायन
भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 एवं 246 में संसद एवं राज्य विधानमण्डलों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है लेकिन इन दोनों अनुच्छेदों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकें कि विधायिका द्वारा विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है।
संविधान में ऐसे अनेक उपबन्ध है जो कार्यपालिका को विधायी निर्माण की शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जैसे –
(i) जब संसद सत्र में नहीं होती है तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश (Ordinance) जारी किया जा सकता है।
(ii) इसी प्रकार जब राज्य विधायिका सत्र में नहीं होती है तब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, तथा
(iii) आपातकाल के दौरान कार्यपालिका द्वारा विधि-निर्माण का कार्य किया जाता है।
यह उपबन्ध संविधान में इसलिए रखे गये क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा प्रत्यायोजित विधायन को आवश्यक समझा गया था।
उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि विधायिका द्वारा विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन एक निर्धारित सीमा तक किया जा सकता है|
यह भी जाने – न्यूसेंस क्या है: परिभाषा एंव इसके आवश्यक तत्व | Essential Elements Of Nuisance
इसके अलावा विधायिका द्वारा ऐसे कृत्यों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है, जो –
(i) आवश्यक प्रकृति के है
(ii) नीति निर्धारण विषयक है
(iii) तात्विक विषयों से सम्बन्धित है, तथा
(iv) विधायी शक्तियों का अभ्यर्पण अथवा परित्याग करने वाले नहीं है।
भारत में प्रत्यायोजित विधायन के विकास के तत्व
भारत में प्रत्यायोजित विधायन के उद्भव एवं विकास का श्रेय इसके लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) के स्वरूप को जाता है। जब राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी नहीं था तब विधायिका के पास कार्यों की अधिकता नहीं थी और अपने सभी विषयों पर वह विधियों का निर्माण कर लेती थी।
लेकिन जैसे-जैसे लोक कल्याणकारी राज्य के नाते इसके कार्यों में अभिवृद्धि होती गई वैसे-वैसे इस पर विधि-निर्माण का बोझ भी बढ़ता गया और इस तरह प्रत्यायोजित विधायन का जन्म हुआ।
भारत में प्रत्यायोजित विधायन के उद्भव एवं विकास के अनेक कारण रहे है या ऐसा कहा जा सकता है कि इसके विकास में अनेक सहयोगी तत्वों की भागीदारी रही है, जिनमे प्रमुख तत्व निम्न है –
(i) समय का अभाव
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संसद के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। संसद के पास केवल विधि निर्माण का कार्य ही नहीं रह गया है अपितु उसे अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार भी करना होता है।
साथ ही बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियों का विनियमन एवं नियन्त्रण का कार्य भी संसद को ही सम्पन्न करना होता है। ऐसी स्थिति में संसद के पास विधि निर्माण के लिए बहुत कम समय बचता है।
इसी कारण संसद द्वारा तात्विक विधियों का निर्माण कर दिया जाता है और उन विधियों के क्रियान्वयन के लिए अनुपूरक विधियाँ, उप विधियाँ, नियम, विनियम आदि बनाने का कार्य कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि संसद के पास समय के अभाव के कारण प्रत्यायोजित विधायन को पल्लवित एवं पुष्पित होने का अवसर मिला है।
(ii) विषय-वस्तु का तकनीकीपन
बीसवीं सदी का उत्तरार्द्ध एवं इक्कीसवीं सदी का प्रारम्भ विशिष्टियों भरा रहा है। आज ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है।
अन्तरिक्ष, परमाणु शक्ति, ऊर्जा, कम्प्यूटर, दूरसंचार आदि प्रौद्योगिकीयों में विश्व कदम बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में इनको विनियमित करने वाली विधियों की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी।
संसद इन सभी विषयों पर समुचित विधियों का निर्माण कर लें, यह आवश्यक नहीं है। संसद में सभी विषयों के विशेषज्ञ उपलब्ध होना भी अनिवार्य नहीं है।
ऐसी स्थिति में ऐसे तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर विधि निर्माण का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाता है। विधायिका ऐसे विषयों पर नीति-निर्धारित कर लेती है और शेष कार्य प्रशासन के जिम्मे छोड़ देती है।
अन्ततः संसद द्वारा उन पर चर्चा एवं विचार-विमर्श कर लिया जाता है। इस प्रकार विषयों का तकनीकीपन प्रत्यायोजित विधायन के विकास का दूसरा कारण रहा है।
यह भी जाने – साक्ष्य कानून में सह अपराधी कौन है? साक्ष्य में उसकी स्थिति और कथन का क्या महत्त्व है?
(iii) लचीलापन
विधि वही अच्छी मानी जाती है जो समय के अनुकूल हो तथा जिसमें देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होने की क्षमता हो। जिस प्रकार जीवन परिवर्तनशील होता है, उसी प्रकार विधियाँ भी परिवर्तनशील होनी चाहिए। यही कारण है कि विधियों में समय–समय पर परिवर्तन, संशोधन आदि करना आवश्यक हो जाता है।
परिवर्तन एवं संशोधन की यह प्रक्रिया प्रत्यायोजित विधायन में आसानी से प्रयोग में लाई जा सकती है यानि नियमों, विनियमों आदि में संशोधन करना आसान है जबकि तात्विक विधियों में बार-बार संशोधन एवं परिवर्तन करना अत्यन्त कठिन है।
(iv) आपात स्थिति
आपात स्थिति एवं आकस्मिकताओं से निपटने के लिए भी प्रत्यायोजित विधायन सार्थक सिद्ध रहा है। कई बार अकस्मात् आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होती है। ऐसी आपात स्थिति युद्ध, बाहरी आक्रमण, अकाल, बाढ़, सूखा, संक्रामक रोग, भूकम्प, आर्थिक संकट आदि किसी भी रूप में हो सकती है।
इन आपात स्थितियों का सामना करने के लिए त्वरित कार्यवाही के अधीन विधि-निर्माण आदि करना होता है। कई महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लेने होते है और उन्हें गोपनीय भी रखना होता है।
इन सबके लिए संसद उपयुक्त स्थान नहीं है फिर कई बार ऐसे समय संसद सत्र में भी नहीं होती है। ऐसी दशा में प्रत्यायोजित विधायन के अधीन प्रशासनिक निर्णय काफी महत्त्वपूर्ण साबित होते है।
प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पारित डिफेन्स ऑफ रेल्म्स एक्ट, 1914 एवं इमरजेन्सी पावर्स एक्ट, 1920 काफी सार्थक साबित हुए है। भारत में भारत रक्षा अधिनियम, 1971 इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
यह ऐसे विधायन है जिनके अधीन कार्यपालिका को व्यापक शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है। इस प्रकार आपात स्थिति का भी प्रत्यायोजित विधायन के विकास में अनुकरणीय योगदान माना जाता है।
(v) स्थानीय एवं क्षेत्रीय विषय
स्थानीय एवं क्षेत्रीय विषयों एवं समस्याओं पर विधि निर्माण के लिए ऐसे व्यक्तियों एवं निकायों की आवश्यकता होती है जो इन विषयों एवं समस्याओं से भली-भाँति परिचित हो एंव इसके साथ ही हितबद्ध व्यक्तियों के परामर्श की भी आवश्यकता होती है।
यह कार्य प्रशासन द्वारा ही भली-भाँति सम्पन्न किया जा सकता है। विधायिका द्वारा पारित तात्विक विधि के अन्तर्गत ऐसे विषयों एवं समस्याओं से निपटने के लिए कार्यपालिका अथवा प्रशासन को नियम, विनियम आदि बनाने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर दी जाती है।
(vi) प्रयोगात्मक कृत्यों का सम्पादन
कतिपय अधिनियमों में कुछ उपबन्ध ऐसे होते हैं जिन्हें किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में किसी तिथि विशेष को लागू करना होता है। इनक नै प्रयोज्यता की तिथि उनकी उपयोगिता के अनुरूप सुनिश्चित की जाती है। यह कार्य सामान्यतया शासन-प्रशासन पर छोड़ दिया जाता है।
शासन-प्रशासन ही यह तय करता है कि किन-किन उपबन्धों को किन-किन क्षेत्रों में कब-कब से लागू किया जाना है। इस प्रकार यह व्यवस्था भी प्रत्यायोजित विधायन के उपयोग एवं महत्त्व को बढ़ा देती है। इसे हम प्रत्यायोजित विधायन के विकास का एक कारण मान सकते हैं।
कई शासकीय एवं प्रशासकीय कार्य इस स्वरूप के होते हैं कि उनके सम्पादन में विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। सामान्यतया लोकोपयोगी सेवायें (Public utility services) इसी प्रकृति की होती है।
ऐसे विषयों पर विधियों, उप-विधियों, नियमों, विनियमों आदि का बनाया एवं जारी किया जाना शासन एवं प्रशासन के लिए ही आसान होता है। इससे भी प्रत्यायोजित विधायन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला।
रमेश बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई. आर. 1990 एस.सी. 56) के मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि, प्रत्यायोजित विधायन का विकास वस्तुतः सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के कारण हुआ क्योंकि इनकी पूर्ति करने के लिए विधानमण्डल व्यापक और विस्तृत विधान बनाने में असफल रहे।
अब स्थिति यह है कि विधायिका साधारण तौर पर विधान में सामाजिक-आर्थिक नौतियों को समाहित कर देती है और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक नियम आदि बनाने का कार्य प्रशासन को सौंप देती है।
इस तरह यह कहा जा सकता है कि, प्रत्यायोजित विधायन वर्तमान समय के लिए अपरिहार्यता बन गया है और इसके बिना एक तरह से विधायिका अपूर्ण है|
महत्वपूर्ण आलेख
अपकृत्य तथा अपराध मै प्रमुख अंतर | Difference Between Tort And Crime
सुने जाने के अधिकार का सिद्धांत | महत्त्व एंव आवश्यक तत्व | Locus Standi in hindi
परिवाद क्या है? परिभाषा, इसके आवश्यक तत्व एंव परिवाद दर्ज करने की प्रक्रिया
नोट – पोस्ट में संशोधन की आवश्यकता होने पर जरूर शेयर करें और ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।
संदर्भ – बुक प्रशासनिक विधि (डॉ. गंगा सहाय शर्मा)