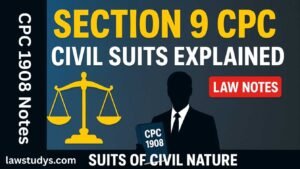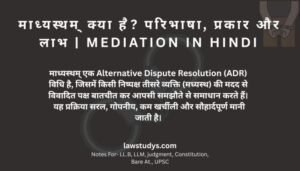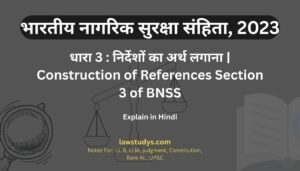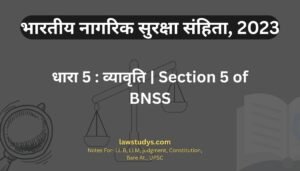नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में विधिशास्त्र के तहत विधिक / कानूनी अधिकारों का वर्गीकरण | Classification of Legal Right in Hindi के बारें में बताने का प्रयास किया गया है, उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा|
कानूनी अधिकार
कानूनी अधिकार (legal right) और क़ानूनी कर्तव्य (legal duty) दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है यानि कानूनी अधिकार एंव कर्तव्य एक ही नियम एंव घटनाओं के अलग – अलग रूप है| सभी विधिशास्त्रियों का मत हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती कर्तव्य जुड़ा रहता है और इन दोनों के अलग अलग अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती|
कानूनी अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे के सहवर्ती निरूपित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है यानि स्वस्थ जीवन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का कानूनी अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था करे।
यह भी जाने – विधिक अधिकार क्या है? अर्थ, परिभाषा, आवश्यक तत्व एंव प्रमुख सिद्वान्त – विधिशास्त्र
कानूनी अधिकारों का वर्गीकरण
कानूनी अधिकारों को मुख्यतः निम्नलिखित भागो में विभाजित किया जा सकता है
पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार
पूर्ण अधिकार से आशय ऐसे अधिकार से है जिसमें हस्तक्षेप या उल्लंघन किये जाने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में सफलतापूर्वक वाद संस्थित किया जा सकता है या अन्य कोई वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है|
जबकि अपूर्ण अधिकार वह होता है जिसे विधि के अन्तर्गत मान्यता तो प्राप्त होती है लेकिन विधि द्वारा उसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। अपूर्ण अधिकार के बारें में एलेन बनाम वाटर्स एण्ड कं. के मामले में कहा गया है की “यह विधि द्वारा मान्य तो होता है लेकिन उसके प्रवर्तन के लिए न्यायालय में वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है| (1935 1 के बी 200)
अपूर्ण अधिकार का अच्छा उदाहरण – “परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा अवधि बाधित ऋण” है। इसमें ऋण समाप्त नहीं होता लेकिन परिसीमा यानि निर्धारित समय अवधी बीत जाने पर उसकी वसूली के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। अवधि बीत जाने से अधिकार का लोप नहीं होता बल्कि उसके लिए उपचार का लोप हो जाता है।
यह भी जाने – 1726 का चार्टर एक्ट एंव इसके प्रावधान | CHARTER ACT OF 1726 – भारत का इतिहास
सकारात्मक व नकारात्मक अधिकार
सकारात्मक अधिकार, सकारात्मक कर्त्तव्य (positive duty) के समरूप या अनुरूप होता है| यह एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति जिसके ऊपर कोई कर्तव्य आरोपित है, अधिकार के धारणकर्ता के लिए कोई कार्य करने के लिए बाध्य होता है।
जबकि नकारात्मक अधिकार, नकारात्मक कर्त्तव्य के समरूप है, अर्थात इसमें कर्त्तव्य से आबद्ध व्यक्ति ऐसे कार्य करने से विरत रहेगा (refrain) जो अधिकार के धारणकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।
उदहारण – किसी लेनदार का ऋणी से ऋण वसूल करने का अधिकार सकारात्मक अधिकार है जबकि जिस व्यक्ति के पास पहले से ही जो कुछ है उसे बनाये रखने का अधिकार नकारात्मक अधिकार है, जैसे – किसी व्यक्ति की जेब में रखे हुए धन के प्रति उसका यह अधिकार कि अन्य व्यक्ति उसे अकारण न छीन ले|
यह भी जाने – न्यूसेंस क्या है: परिभाषा एंव इसके आवश्यक तत्व | Essential Elements Of Nuisance In Hindi
सर्वबन्धी तथा व्यक्तिबन्धी अधिकार
सर्वबन्धी कानूनी अधिकार सामान्यत: व्यक्तियों पर अधिरोपित कर्तव्यों के साथ चलते हैं जबकि व्यक्तिबन्धी अधिकार निश्चित व्यक्तियों पर अधिरोपित कर्त्तव्य के साथ चलते हैं। सर्वबन्धी अधिकार समस्त संसार के व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोज्य होते हैं जबकि व्यक्तिबंधी अधिकार केवल विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध ही प्रयोज्य हैं।
प्रत्येक व्यक्ति का अपने निवास गृह में रहने का अधिकार सर्वबन्धी अधिकार है क्योंकि समस्त व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि वे किसी के उक्त अधिकार में हस्तक्षेप न करें। लगभग सभी सर्वबन्धी अधिकार नकारात्मक होते हैं जबकि अधिकांश व्यक्तिबन्धी अधिकार सकारात्मक होते हैं।
साम्पत्तिक तथा वैयक्तिक अधिकार
साम्पत्तिक अधिकार मनुष्य की सम्पत्ति या सम्पदा में निहित होते हैं और इसका सम्बन्ध व्यक्ति की संपत्ति, उसकी आस्तियों (assets) अथवा कीर्तिस्व आदि से होता हैं।
इसी प्रकार मनुष्य के वैयक्तिक अधिकारों का सम्बन्ध उसके व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा या हैसियत (status) से होता है। वैयक्तिक अधिकार अन्तरणीय नहीं होते है तथा व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् पूर्णत: समाप्त हो जाते हैं।
उदाहरण – किसी व्यक्ति को पिता या पति की हैसियत से जो अधिकार अपने बच्चों या पत्नी के प्रति प्राप्त हैं, वे उसके वैयक्तिक अधिकार होते हैं।
सामंड ने साम्पत्तिक अधिकार को मूल्यवान अधिकार माना है जबकि वैयक्तिक अधिकार को साम्पत्तिक अधिकार से कम मूल्यवान माना है|
स्व–साम्पत्तिक तथा पर–साम्पत्तिक अधिकार
किसी व्यक्ति का उसकी निजी सम्पत्ति पर अधिकार, स्व-साम्पत्तिक (Right in re-propria) कहलाता है जबकि किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर अधिकार रखना पर-साम्पत्तिक अधिकार (Right in re-aliena) कहलाता है।
उदाहरण – किसी व्यक्ति का अपनी भूमि पर स्व-साम्पत्तिक अधिकार होता है और ऐसी भूमि पर आने-जाने के लिए पड़ोसी की भूमि के मार्गाधिकार पर उसका पर-साम्पत्तिक अधिकार होगा। पर-साम्पत्तिक अधिकार को विल्लंगम (encumbrance) भी कहते है।
- सामण्ड ने विल्लंगम के चार मुख्य प्रकार बताये हैं
(i) पट्टा (Lease) – पट्टे में सम्पत्ति का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति में निहित रहता है जबकि उस सम्पत्ति का कब्जा तथा उपयोग किसी अन्य व्यक्ति में निहित होता है। स्वामित्व (ownership) और आधिपत्य (possession) के न्यायोचित बंटवारे को पट्टा या लीज कहते हैं।
(ii) सुविधाभार (Servitude) – सुविधाभार में व्यक्ति को केवल भूखण्ड के सीमित उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है तथा स्वामित्व तथा कब्जा उसे अन्तरित नहीं किया जाता। सुविधाभार सम्बन्धी अधिकार या तो सामूहिक या व्यक्तिगत हो सकता है।
(iii) प्रतिभूति (Security) – प्रतिभूति एक ऐसा भार (charge) या विल्लंगम है जो किसी लेनदार को उसके ऋणी की सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है ताकि ऋण की वसूली की सुरक्षा बनी रहे। प्रतिभूति या तो बन्धक के रूप में हो सकती है या धारणाधिकार के रूप में।
(iv) न्यास (Trust) – न्यास एक ऐसा विल्लंगम है जिसमें सम्पत्ति का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए साम्यिक बाध्यता द्वारा सीमित होता है।
उदाहरण – यदि एक व्यक्ति अपनी कोई सम्पत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हित या लाभ के लिए तीसरे व्यक्ति को सौंपता है, तो यहाँ न्यास का निर्माण हुआ है तथा वह तीसरा व्यक्ति उस सम्पत्ति का न्यासी कहलायेगा, जिस व्यक्ति के हित के लिए न्यास निर्मिति होती है उसे हितग्राही (Beneficiary) कहते हैं।
प्रधान तथा सहायक अधिकार
प्रधान अधिकार का अस्तित्व अन्य अधिकारों से स्वतन्त्र होता है, परन्तु सहायक अधिकार (accessory rights), प्रधान अधिकार के अनुषंगी अधिकार होता हैं।
उदाहरण – यदि कोई ऋण बन्धक द्वारा प्रतिभूत है तो वह ऋण प्रधान अधिकार होगा और प्रतिभूति सहायक अधिकार होगा। इसी प्रकार यदि किसी खेत के मालिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस खेत से लगे दूसरे खेत में होकर जा सकता है, तो यहाँ पहले खेत का स्वामित्व प्रधान अधिकार होगा और दूसरे खेत में से होकर जाने का अधिकार सहायक अधिकार होगा।
विधिक तथा साम्यिक अधिकार
इंग्लैंड में सन् 1873 का जूडीकेचर एक्ट पारित होने से पूर्व कानूनी अधिकार से आशय ऐसे अधिकार से है जो इंग्लैण्ड के कॉमन लॉ द्वारा मान्य थे, जबकि साम्यिक अधिकार (equitable rights) केवल चांसरी न्यायालय द्वारा मान्य किये गये थे।
साम्यिक अधिकार आंग्ल विधि के देन है, भारत में विधि एंव साम्य में कोई भेदभाव नहीं किया गया है| इस सम्बन्ध में प्रिवी कौंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि भारत में ‘सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882’ पारित हो जाने के बाद विधिक तथा साम्यिक अधिकार व हितों में कोई भेद नहीं रह गया है।
विधिक और साम्यिक अधिकार एक दूसरे से निम्नलिखित बातों में भिन्न हैं –
(i) विधिक तथा साम्यिक अधिकारों के सृजन एवं व्ययन की रीति भिन्न-भिन्न होती है।
(ii) साम्यिक अधिकार की तुलना में विधिक अधिकार को अधिमान्यता प्राप्त है क्योंकि ये अधिकार साम्यिक अधिकारों से गुरुतर होते हैं।
(iii) साम्यिक अधिकारों की तुलना में विधिक अधिकार अधिक सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित होते हैं।
प्राथमिक तथा शास्तिक अधिकार
प्राथमिक अधिकार को पूर्ववर्ती या सारभूत अधिकार भी कहा जाता है। इसी प्रकार शास्तिक अधिकार को उपचारात्मक या अनुपूरक, द्वितीयक अधिकार भी कहते हैं।
प्राथमिक अधिकार स्वतंत्र अस्तित्व वाले अधिकार होते है, प्राथमिक अधिकार का स्रोत अपकृत्य (wrong) के अलावा अन्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन शास्तिक अधिकार किसी प्राथमिक अधिकार के उल्लंघन या अतिक्रमण से ही उत्पन्न होता है।
उदहारण – ‘क’ एक भूमि का स्वामी है जिसे अधिकार है कि वह अपनी भूमि का स्वतंत्र उपयोग उपभोग करे, यह उसका प्राथमिक अधिकार है और अब ‘ख’ यदि ‘क’ की भूमि पर अतिक्रमण करता है तब उस स्थिति में ‘ख’ के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाने के लिए ‘क’ का अधिकार द्वितीयक या उपचारात्मक अधिकार है।
लोक अधिकार तथा प्राइवेट अधिकार
ऐसे अधिकार जो राज्य में निहित होते हैं, लोक अधिकार कहलाते हैं। राज्य इन अधिकारों को लोक प्रतिनिधि की हैसियत से प्रजा के हित के लिए प्रवर्तित कराता है तथा ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों में निहित होते हैं प्राइवेट अधिकार कहलाते हैं।
ब्लैकस्टोन (Blackstone) ने अपकृत्यों (wrongs) का (i) लोक-अपकार तथा (ii) वैयक्तिक अपकार में विभाजन, इन दो अधिकारों के आधार पर ही किया है।
उदाहरण – व्यक्ति का अपनी भूमि का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करने का कानूनी अधिकार एक लोक अधिकार है परन्तु यही भूमि किराये या पट्टे पर दे दी जाती है उस स्थिति में किरायेदार से किराया वसूल करने का अधिकार प्राइवेट अधिकार बन जाता है|
निहित तथा समाश्रित अधिकार
निहित अधिकार (vested right) से तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जिसमें अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी शर्ते घटित हो चुकती हैं।
जबकि समाश्रित अधिकार वह है जिसके सम्बन्ध में अधिकार निहित करने के लिए केवल कुछ शर्ते घटित होती हैं और कुछ शर्तों का पूरा होना किसी अनिश्चित घटना के घटित होने अथवा न होने पर निर्भर करता है। ऐसी घटना के घटित होने या न होने पर समाश्रित अधिकार पूर्ण होकर निहित अधिकार में परिवर्तित हो जाता है।
उदाहरण – यदि कोई व्यक्ति किसी विलेख द्वारा अपनी सम्पत्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को अन्तरित करता है, तो दूसरे व्यक्ति को उस सम्पत्ति पर निहित अधिकार प्राप्त होगा। परन्तु यदि सम्पत्ति का अन्तरण किसी अजन्मे बालक के हक में किया जाता है, तो वह अजन्मा बालक केवल समाश्रित अधिकार अर्जित करेगा, जिसका निहित अधिकार में परिवर्तित होना उस अजन्मे बालक के जन्म लेने तथा जीवित रहने पर निर्भर करता है।
अधिसेवी तथा अधिभावी अधिकार
अधिसेवी कानूनी अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी विल्लंगम के अधीन होता है। परन्तु जब ऐसे अधिकार में से विल्लंगम हट जाता है, तो वह अधिभावी अधिकार का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। वह भूमि जिसके फायदेमंद उपभोग के लिए अधिकार अस्तित्व में है, अधिभावी दाय कहलाती है तथा उस भूमि के स्वामी को अधिभावी स्वामी कहते हैं।
इसके विपरीत, वह भूमि, जिस पर दायित्व अधिरोपित किया जाता है, अधिसेवी दाय (servient heritage) कहलाती है और ऐसी भूमि का स्वामी अधिसेवी स्वामी कहलाता है।
उदाहरण – यदि किसी मकान के स्वामी के नाते ‘अ’ को अपने पड़ोसी ‘ब’ की भूमि पर से आने-जाने का सुखाधिकार प्राप्त है, तो ‘अ’ का मकान अधिभावी दाय होगी और ‘अ’ उसका अधिभावी स्वामी कहलायेगा; तथा ‘ब’ का मकान अधिसेवी दाय होगी व उस मकान के स्वामी के नाते ‘ब’ को अधिसेवी स्वामी कहा जायेगा।
नगरीय अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार
नगरीय अधिकार (Municipal Rights) देशवासियों को देश की विधि द्वारा प्रदत्त किये जाते हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त किया जाता है।
अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकारों के संबंध में एक धारणा यह है कि केवल राज्य ही इसकी विषय-वस्तु होने के कारण ये कानूनी अधिकार केवल राज्य को ही प्रदत्त किये जा सकते हैं न कि व्यक्तियों को। परन्तु कुछ विद्वान इस धारणा को उचित नहीं मानते क्योंकि उनके विचार से ‘व्यक्ति’ भी अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार की विषय-वस्तु हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण आलेख
सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार एंव इसके विभिन्न प्रकार। Jurisdiction of Civil Courts
आरोपों का संयोजन, कुसंयोजन एंव इसके अपवाद | आरोप की विरचना | धारा 218 से 223 CrPC
CePC 1973 के अन्तर्गत अभियुक्त के अधिकार (Rights of the Accused) की विवेचना